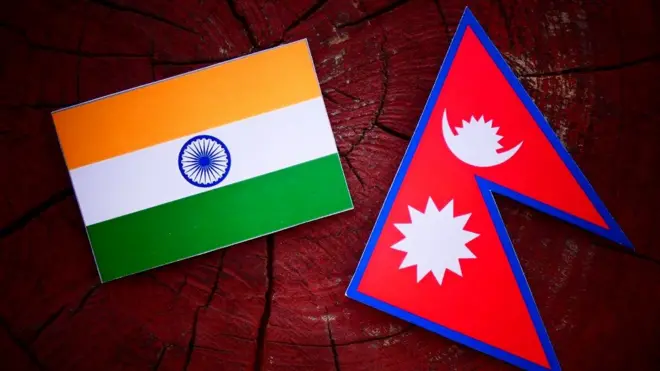क्या भारत से पड़ोसी देश दूर होते जा रहे हैं?

इमेज स्रोत, Reuters
- Author, शुभज्योति घोष
- पदनाम, बीबीसी न्यूज बांग्ला, दिल्ली
- पढ़ने का समय: 18 मिनट
क़रीब दस साल पहले नरेंद्र मोदी ने जब पहली बार भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली थी तो उन्होंने तमाम पड़ोसी देशों की सरकारों या राष्ट्र के प्रमुखों को भारत आने का न्योता देकर सबको चौंका दिया था.
यहां तक कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज़ शरीफ़ को भी इस मौके पर आने का न्योता दिया गया था.
मोदी सरकार पहले दिन से ही कहती रही है कि भारत की विदेश नीति में पड़ोसी देशों को सबसे ज़्यादा महत्व मिलेगा.
इसी नीति को औपचारिक तौर पर 'नेबरहुड फ़र्स्ट' या 'पड़ोसी सबसे पहले' नाम दिया गया है. दिल्ली में सरकार के मंत्री या नीति निर्धारक बीते एक दशक से बार-बार कहते रहे हैं कि यही नरेंद्र मोदी सरकार की विदेश नीति का मूल आधार है.
इसे दूसरे शब्दों में कहें तो 'नेबरहुड फ़र्स्ट' की मूल बात यह है कि भारत भौगोलिक रूप से दूर (वह चाहे अमेरिका हो या नाइजीरिया) के मुकाबले दक्षिण एशिया के पड़ोसी देशों (श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार और नेपाल आदि) के साथ संबंधों को ज़्यादा अहमियत देगा और उनके हितों को प्राथमिकता देगा.
लेकिन ज़ुबानी कहना और बात है. पर क्या हक़ीकत में भी नरेंद्र मोदी सरकार के कामकाज में इसकी झलक मिलती है?
एक ओर जहां दिल्ली ने अक्सर पश्चिमी देशों को ज़्यादा महत्व दिया है, वहीं वह चीन को लेकर भी ज़्यादा सिर खपाती रही है.

इमेज स्रोत, Getty Images


इमेज स्रोत, Getty Images
दूर होते पड़ोसी देश
प्रधानमंत्री के तौर पर अपने पहले दौरे के दौरान (नेपाल) अगस्त, 2014), श्रीलंका (मार्च, 2015) और बांग्लादेश (जून, 2015) में नरेंद्र मोदी का जिस तरह बड़े पैमाने पर स्वागत किया गया था और आम लोगों की शानदार प्रतिक्रिया मिली थी, उन देशों में बाद में तस्वीर वैसी नहीं नज़र आई.
पाकिस्तान के साथ संबंधों में भी बेहतरी के कोई लक्षण नहीं नज़र आए.
अब नेबरहुड फ़र्स्ट के एक दशक बाद देखने में आ रहा है कि भारी आर्थिक संकट के दौर में भारत ने जिस श्रीलंका की काफी मदद की थी, वहां की सरकार ने भी दिल्ली की टेढ़ी निगाहों को नज़रअंदाज़ कर चीन के जासूसी जहाज को अपने बंदरगाह पर लंगर डालने की अनुमति दे रही है.
नेपाल में नए संविधान को लागू करने के दौरान भारत के मौन समर्थन से चलाए गए 'आर्थिक नाकेबंदी' कार्यक्रम के ख़िलाफ़ नेपाल की आम जनता भारत विरोधी प्रदर्शनों में शामिल हो गई.
फ़िलहाल नेपाल की सत्ता में केपी शर्मा ओली को भी कट्टर भारत विरोधी ही माना जाता है.
मालदीव में भी बीते साल चुनाव में भारत-समर्थक सरकार को सत्ता से हटा कर राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठने वाले मोहम्मद मुइज़्ज़ू ने तुरंत अपने देश से भारतीय सेना को हटाने की मांग उठा दी.
उनकी पार्टी की ओर से चलाए गए 'इंंडिया आउट' अभियान को काफ़ी समर्थन मिला है और राष्ट्रपति मुइज़्ज़ू बिना किसी हिचकिचाहट के चीन की ओर झुक रहे हैं.
यहां तक कि जो भूटान सामरिक, विदेशी और आर्थिक, लगभग तमाम मामलों में भारत पर निर्भर है, उसने भी अकेले अपने दम पर चीन के साथ सीमा पर बातचीत शुरू कर दी है.
उसने कूटनयिक संबंध स्थापना के चीन के प्रस्ताव को भी सीधे तौर पर ख़ारिज़ नहीं किया है.

इमेज स्रोत, Getty Images
यह भी नहीं कहा जा सकता कि अफ़ग़ानिस्तान और म्यांमार में सत्तारूढ़ सरकार के साथ भी भारत के संबंध अच्छे हैं.
तालिबान के साथ अब तक भारत का पूर्ण कूटनयिक संबंध स्थापित नहीं हो सका है.
इन दोनों देशों में भारत की ओर से विभिन्न क्षेत्रों में किया गया सैकड़ों करोड़ का निवेश भी अब अनिश्चितता के भंवर में फंस गया है.
इस सूची में ताज़ा नाम है बांग्लादेश का, जहां बीते डेढ़ दशक से भारत की एक घनिष्ठ मित्र सरकार के सत्ता में रहने के बाद लगभग रातों रात उसे सत्ता छोड़नी पड़ी.
उसके बाद वहां सत्ता में ऐसी कुछ ताक़तें शामिल हो गई हैं जिनको भारत का मित्र नहीं कहा जा सकता.
इसके अलावा क़रीब साढ़े तीन साल पहले नरेंद्र मोदी के बांग्लादेश दौरे के दौरान ही उनके ख़िलाफ़ विरोध प्रदर्शन और हिंसा चरम पर थी.
तमाम पर्यवेक्षक इस बात को मानते हैं कि बांग्लादेश में हाल के आरक्षण विरोधी आंदोलनों में भी प्रबल भारत विरोधी भावना शामिल थी.
तो क्या भारत की विदेश नीति में ऐसी कुछ गंभीर खामियां हैं जिसकी वजह से एक के बाद एक पड़ोसी देशों में भारत-विरोधी भावनाएं सिर उठा रही हैं?
या फिर दक्षिण एशिया की भू-राजनीतिक संरचना ही ऐसी है कि भारत के लिए यह नियति पहले से तय थी?
इन सवालों के जवाब तलाशने के लिए बीबीसी बांग्ला ने भारत और भारत के बाहर अंतरराष्ट्रीय संबंध विश्लेषकों, प्रोफेसरों, पूर्व राजदूतों और कूटनीति मामले के विशेषज्ञों से विस्तार से बात की.
इस रिपोर्ट में उन तमाम लोगों की टिप्पणियों को शामिल किया गया है.

ये रिपोर्ट्स भी पढ़िए-

भारतीय विदेश नीति में अल्पकालिक हितों को प्राथमिकता
इरफ़ान नूरुद्दीन

इमेज स्रोत, Wilson Center
डॉ. इरफान नूरुद्दीन अमेरिका के वाशिंगटन में जार्जटाउन यूनिवर्सिटी के स्कूल आफ़ फ़ॉरेन सर्विस में भारतीय राजनीति के प्रोफ़ेसर है. वो आर्थिक विकास, वैश्वीकरण, लोकतंत्र और लोकतंत्रीकरण और नागरिक संघर्ष पर शोध करते हैं.

पहले ही कहना चाहूंगा कि दक्षिण एशिया दुनिया का सबसे कम एकीकृत (लिस्ट इंटीग्रेटेड) क्षेत्र है. यहां एक देश से दूसरे देश में आवाजाही या अंतरराष्ट्रीय सीमा संबंध जितने कठिन और जटिल हैं, उतना दुनिया के किसी और इलाक़े में नहीं हैं.
अगर वाणिज्य की बात करूं तो सब-सहारा क्षेत्र के ग़रीब अफ़्रीकी देशों के बीच भी जिस मात्रा में अंतर-क्षेत्रीय व्यापार होता है उसके मुक़ाबले दक्षिण एशियाई देशों में आपसी व्यापार की मात्रा कम है.
हालांकि इस इलाक़े में स्थित देशों में दो अरब या 200 करोड़ से ज़्यादा लोग रहते हैं और यह दुनिया का एक प्रमुख आर्थिक केंद्र ( इकोनॉमिक हब) बन सकता था.
इसलिए किसी को यह समझने के लिए रॉकेट वैज्ञानिक होने की ज़रूरत नहीं है कि क्षेत्र के सबसे बड़े और सबसे प्रभावशाली देश के बीच संबंध सहज और स्वाभाविक नहीं हैं.
भारत की विदेश नीति का विश्लेषण करने पर पता चलता है कि भारत मालदीव, श्रीलंका या नेपाल जैसे किसी भी पड़ोसी देश के साथ दीर्घकालिक संबंध स्थापित करने के मक़सद से किसी बहुआयामी नीति के साथ कभी आगे नहीं बढ़ा है.
इस मामले में हमेशा अल्पकालिक हितों या 'शार्ट टर्म इंटरेस्ट' को प्राथमिकता दी गई है. इसी वजह से इसके लिए एक संकीर्ण और संदिग्ध एक-आयामी नीति अपनाई गई है.
भारत की मौजूदा सरकार अपनी 'हिन्दू पहचान' को अपनी विदेश नीति के प्रमुख स्तम्भ के रूप में स्थापित करना चाहती है और बांग्लादेश जैसे कई मुस्लिम-बहुल देशों में इसका हमेशा की तरह उल्टा असर हुआ है.
नरेंद्र मोदी सरकार की ओर से लागू नागरिकता कानून का मूल मक़सद ही भारत को हिंदुओं की अंतिम शरणस्थली के तौर पर पेश करना था.
भारत के नेता और मंत्री लगातार अवैध मुस्लिम घुसपैठियों के लिए 'बांग्लादेशी' शब्द का इस्तेमाल करते रहे हैं और दूसरी ओर वो बांग्लादेश के साथ संबंधों में काफ़ी मजबूती आने का भी दावा करते रहे हैं.
लेकिन इन दोनों बातों में घोर परस्पर विरोधाभास है जिसे ज़्यादा दिनों तक दबा कर रखना संभव नहीं हो सका है.
इस संदर्भ में यह भी कहना चाहूंगा कि बीते एक दशक के दौरान हमने भारत के कई पड़ोसी देशों में देखा है कि वहां की सरकार तो भारत के प्रति काफ़ी मित्रतापूर्ण रवैया अपनाती रही है लेकिन वहां के आम लोग भारत विरोधी भावनाओं से उबल रहे हैं.
बांग्लादेश के अलावा नेपाल और मालदीव में यही बात देखने को मिली है.
लेकिन स्थिरता या लोकतंत्र की ख़ातिर भारत ने कभी भी उन देशों के लोगों की नाराज़गी को दूर करने का कोई प्रयास नहीं किया.
उल्टे उसने मान लिया है कि उन देशों की सरकारें के साथ रहने पर उसके (भारत के) हित सुरक्षित रहेंगे.
इसकी वजह भी साफ़ है जिसका ज़िक्र मैं पहले भी कर चुका हूं.
भारत हमेशा पड़ोसी देशों में अपने अल्पकालिक हितों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ा है, उसने दीर्घकालिक हितों के बारे में कभी माथापच्ची नहीं की है.
उसे एक के बाद एक तमाम देशों में इसका नतीजा भी भुगतना पड़ रहा है.
ऐसे में दक्षिण एशिया के छोटे देश अगर भारत को एक क्षेत्रीय आधिपत्य ताक़त के रूप में देखते हैं तो उसका एक निर्धारित दृष्टिकोण और कारण है.
यह तो समझ में आता है कि भारत खुद को एक क्षेत्रीय महाशक्ति के तौर पर स्थापित करना चाहता है.
लेकिन ऐसा करने की स्थिति में उसे इन पड़ोसी देशों के प्रति कुछ ज़िम्मेदारियों का भी पालन करना होगा और एक बहुआयामी संबंध कायम होगा. फ़िलहाल यह कहीं नज़र नहीं आता.
भारत की विदेश नीति की असफलता
एस डी मुनि

इमेज स्रोत, SD MUNI
डॉ. मुनि दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू और सिंगापुर नेशनल यूनिवर्सिटी समेत दुनिया के कई शैक्षणिक संस्थानों में अंतरराष्ट्रीय संबंधों के प्रोफ़ेसर रह चुके हैं. उन्होंने दक्षिण पूर्व एशिया में भारत के विशेष दूत के तौर पर भी काम किया है. वो दिल्ली के थिंक टैंक आईडीएसए से प्रतिष्ठित फेलो के तौर पर भी जुड़े हैं.

नरेंद्र मोदी सरकार ने सत्ता में आने के बाद ही जिस 'नेबरहुड फ़र्स्ट' नीति का एलान किया था उसकी शुरुआत में ही ख़ामी थी.
मैं कहूंगा कि उस एलान से पहले कोई गंभीर सोच-विचार नहीं किया गया था. वह एक औचक लिया गया फैसला था.
मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में सार्क देशों के तमाम नेताओं को आमंत्रित करने के कुछ दिनों बाद ही हमने देखा कि पाकिस्तान से दिल्ली आने वाले एक व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल को कश्मीर के हुर्रियत नेताओं से मुलाक़ात करने की अनुमति ही नहीं दी गई.
हालांकि हुर्रियत के नेता उसी बैठक के लिए पहले से दिल्ली पहुंच कर इंतजार कर रहे थे.
अब अगर हुर्रियत के नेताओं को पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल के साथ मुलाक़ात की अनुमति ही नहीं देनी थी तो उनको श्रीनगर से दिल्ली आने ही नहीं देना चाहिए था.
और अगर भारत, पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत ही नहीं करना चाहता तो मोदी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में नवाज़ शरीफ़ को न्योता भेजने की भी कोई ज़रूरत नहीं थी.
मैं ऐसे कई उदाहरण दे सकता हूं जिससे साफ़ समझा जा सकता है कि पड़ोसी देशों को महत्व देना कभी भी 'नेबरहुड फ़र्स्ट' नीति का मक़सद नहीं रहा.
सीधे शब्दों में कहें तो वह 'नेबरहुड फ़र्स्ट' नहीं बल्कि 'इंडिया फ़र्स्ट' पालिसी थी.
मेरी राय में मोदी के शासनकाल के दौरान भारत ने विदेश नीति लागू करने में दो और गंभीर ग़लतियां कीं.
पहली है ख़ुफ़िया तंत्र पर ज़रूरत से ज़्यादा निर्भरता.
यह ठीक है कि ख़ुफ़िया सूचनाएं ज़रूरी हैं, लेकिन अगर ख़ुफ़िया विभाग की निगाहों से हम किसी पड़ोसी देश को देखने का प्रयास करते हैं और उसी आधार पर नीति या रणनीति बनाते हैं तो जो नतीजा होना चाहिए, वही हुआ है.
दूसरी बात यह है कि मोदी सरकार से पहले हमने कभी नहीं देखा है कि विदेश नीति को लागू करने में सत्तारूढ़ पार्टी को सक्रिय रूप से शामिल किया गया है.
मोदी के पहले या दूसरे शासनकाल में भी विदेश मंत्री की बजाय आरएसएस नेता राम माधव इस बात का फैसला करते थे कि भारत, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार या कुछ हद तक पाकिस्तान के साथ किस नीति पर आगे बढ़ेगा.
पड़ोसी देशों के साथ भारत की रणनीति तय करने की ज़िम्मेदारी भाजपा और आरएसएस के इन नेताओं को ही सौंप दी गई थी.
अब तो यह साफ़ हो गया है कि इसका नतीजा भारत के हित में नहीं रहा.
अगर बांग्लादेश की मौजूदा परिस्थिति की चर्चा करें तो वहां भी भारत की विदेश नीति की विफलता के लिए कई कारणों को ज़िम्मेदार ठहराया जा सकता है.
मिसाल के तौर पर भारत ने कभी भी प्रधानमंत्री शेख़ हसीना को स्पष्ट रूप से इस बात की याद नहीं दिलाई कि वह ठीक रास्ते पर आगे नहीं बढ़ रही हैं और आम लोगों में उनके ख़िलाफ़ नाराज़गी बढ़ रही है.
अगर वो भारत की बेहतर मित्र थीं तो उनको गंभीरता से यह बात बताई जानी चाहिए थी. लेकिन ऐसा नहीं किया गया. इसके अलावा चरम ख़ुफ़िया विफलता तो थी ही.
बंगबंधु शेख़ मुजीब हत्याकांड से पहले भी इंदिरा गांधी के राजनीतिक सचिव पीएन हक्सर ने सुरक्षा के लिहाज से उनको हेलीकॉप्टर के ज़रिए वहां से निकालने का प्रस्ताव दिया था.
यह अलग बात है कि बंगबंधु इसके लिए तैयार नहीं हुए. लेकिन भारत को इस बात की जानकारी थी कि उनके जीवन पर ख़तरा है.
लेकिन भारत को इस बात की भनक तक नहीं मिली कि शेख़ हसीना को सत्ता से हटाए जाने की कोई संभावना है.
मैं तो कहूंगा कि राजनीतिक रूप से शेख़ हसीना का समर्थन कर भारत ने एक ब्लैंक चेक पर हस्ताक्षर कर दिए थे. अब वह दांव उल्टा पड़ा है.
चार पड़ोसी मुल्कों में भारत विरोधी सरकारें
सौमेन राय

इमेज स्रोत, Soumen Roy
सौमेन राय कई देशों में राजदूत भी रहे हैं. मध्य पूर्व और बांग्लादेश उनके शोध और दिलचस्पी के प्रमुख इलाके रहे हैं.

पहले ही एक बात साफ़ तौर पर कहना ज़रूरी है कि भारत के पड़ोसी देशों में होने वाली घटनाओं को मैं भारत की विदेश नीति या 'नेबरहुड फ़र्स्ट' की नाकामी नहीं मानता.
दुनिया के लगभग सभी देश विभिन्न वजहों से राजनीतिक उथल-पुथल के दौर से गुजर रहे हैं. दक्षिण एशिया भी अपवाद नहीं है.
अब नेपाल, मालदीव या बांग्लादेश में अगर राजनीति की तस्वीर बदलती है या सत्ता में नाटकीय बदलाव होता है तो उसके लिए मूल रूप से उन देशों की आंतरिक परिस्थिति ही ज़िम्मेदार है.
मान लेते हैं कि इनमें से किसी देश में कई व्यक्ति लंबे समय से सत्ता में है और उसके ख़िलाफ़ सत्ता विरोधी लहर तेज़ हो रही है.
ऐसी स्थिति में भारत या उसकी विदेश नीति चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती, वह देश अपनी राजनीतिक दशा-दिशा के आधार पर ही आगे बढ़ेगा.
तो क्या मैं यह कहना चाहता हूं कि इन सभी पड़ोसियों के साथ भारत के संबंधों में सब कुछ ठीक-ठाक चल रहा है?
नहीं, यह भी सही नहीं है. इन संबंधों में कई तरह की दरारें हैं और यही कभी कभार बढ़ कर गंभीर समस्याएं पैदा करती हैं.
लेकिन भारत के साथ इन देशों के क्षेत्रफल, सैन्य, आर्थिक शक्ति या वैश्विक प्रभाव में भारी अंतर के कारण यह दरार क़ायम रहेंगी.
भारत और उसके पड़ोसियों को इन वास्तविकताओं के साथ आगे बढ़ना होगा. रिश्तों में उतार-चढ़ाव तो आएंगे ही.
अगर किसी देश में नाटकीय परिवर्तन होता है तो वहां का आंतरिक घटनाक्रम किसी भी अन्य कारक की तुलना में सबसे बड़ी भूमिका निभाता है.
अब अगर मान लें कि काठमांडू, काबुल, माले या ढाका में एक साथ चार भारत-विरोधी सरकार सत्ता में आई हैं तो मैं इसे महज संयोग ही मानूंगा.
विभिन्न देशों के साथ भारत के संबंधों में उतार-चढ़ाव जारी रहेगा. फिलहाल एक साथ तीन या चार देशों के साथ द्विपक्षीय संबंध चुनौतीपूर्ण दौर में हैं. लेकिन ऐसा तो हो ही सकता है.

इमेज स्रोत, Getty Images
लेकिन मैं एक बात याद दिलाना चाहता हूं कि भारत के पड़ोसी देशों में (पाकिस्तान को छोड़ कर) चाहे जो भी सरकार सत्ता में रहे, दिल्ली के साथ उसकी बातचीत का रास्ता कभी बंद नहीं हुआ है.
मालदीव की मुइज़्ज़ू सरकार तक भारत से सहायता मांग चुकी है. हर दौर में नेपाल के साथ सहयोग कायम रहा है.
बांग्लादेश में चाहे जो भी सरकार सत्ता में आए, दिल्ली और ढाका को आपस में संपर्क और सहयोग बना कर चलना ही होगा. इसका उलट कभी विकल्प नहीं हो सकता.
मैं इस 'कामकाजी रिश्ते' को क़ायम रखने को दिल्ली की क़ामयाबी मानता हूं.
बांग्लादेश के संदर्भ में कई लोग भारत की आलोचना करते हुए कहते हैं कि उसने 'तमाम अंडे एक ही टोकरी में' रख दिए थे.
यानी शेख़ हसीना और अवामी लीग पर ही भरोसा जताया था और भारत को आज उसी की क़ीमत चुकानी पड़ रही है.
लेकिन ऐसे लोगों से मेरा सवाल है कि क्या बांग्लादेश में हकीकत में भारत के लिए कभी कोई दूसरी 'टोकरी' थी?
सीधे शब्दों में कहें तो जो राजनीतिक ताक़तें अतीत और वर्तमान में भारत-विरोधी भावनाओं से भरी हैं, उनसे हाथ मिलाना दिल्ली के लिए संभव नहीं था.
अब इसे आप नीति की नाकामी कहें या कुछ और, यही हकीकत है.
संजय के. भारद्वाज

इमेज स्रोत, JNU
दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में सेंटर फॉर साउथ एशियन स्टडीज के साथ लंबे समय से जुड़े संजय भारद्वाज उस संस्थान के चेयरमैन भी रहे हैं. वो लंबे अरसे से पड़ोसी देशों के साथ भारत के संबंधों पर शोध कर चुके हैं और उन्होंने बांग्लादेश में भी लंबा समय गुजारा है.

भारत एक वृहद क्षेत्रीय महाशक्ति है और वह धीरे-धीरे वैश्विक ताकत बनना चाहता है.
उसके इस लक्ष्य तक पहुंचने में पड़ोसी देशों की बड़ी भूमिका है. इसकी वजह यह है कि अपने भौगोलिक इलाके में पड़ोसियों की मान्यता या सम्मान नहीं मिलने की स्थिति में किसी देश के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सम्मान हासिल करना मुश्किल हो जाता है.
भारत की विदेश नीति में यही बात कही गई है. उसमें पड़ोसी देशों को समुचित महत्व देते हुए उनका भरोसा हासिल करने की बात कही गई है.
अब जिस नेबरहुड पॉलिसी की बात कही जा रही है. यह कोई एकदम नई चीज नहीं है.
तीन दशक पहले तत्कालीन प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल ने दक्षिण एशिया में गुजराल डाक्टरीन का पालन करने की बात कही थी. उसकी मूल बात थी गैर-पारस्परिकता. यानी पड़ोसी ने क्या किया या क्या नहीं किया, यह सोचने की बजाय संबंधों में बेहतरी के लिए एकतरफा तरीके से कदम उठाना होगा.
उसके बाद मनमोहन सिंह के दौर में यही बात अलग तरीके से कही गई. तब कहा गया कि पड़ोसी देशों के साथ उदारता बरती जाए. इससे द्विपक्षीय संबंध अपने आप बेहतर हो जाएंगे.
इस संदर्भ में यह याद दिलाना जरूरी है कि बांग्लादेश के साथ ऐतिहासिक जमीन समझौता या प्रस्तावित तीस्ता समझौते का प्रारूप मनमोहन सिंह सरकार के कार्यकाल में ही तैयार किया गया था. बाद में नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में इसे ही नेबरहुड फर्स्ट का नाम दिया गया. लेकिन पड़ोसी देशों के साथ संबंधों का मूल तत्व जस का तस ही है.
अब भारत के साथ एक बड़ी दिक्कत यह है कि वह चीन की तरह पड़ोसी देशों में बड़े पैमाने पर निवेश करने या वहां खैरात चलाने में आर्थिक तौर पर सक्षम नहीं है.
जबकि भारत के लगभग सभी पड़ोसी उभरती अर्थव्यवस्थाएं हैं, उनकी अपनी उम्मीदें और विकास एजेंडा है. उनको पूरा करने के लिए चीन ने उनके लिए अपना खजाना खोल दिया है. यही वजह है कि पड़ोसी देश सांस्कृतिक या भौगोलिक रूप से भारत के जितने भी करीब हों, आर्थिक जरूरत के चलते वो चीन के प्रभाव में आ रहे हैं. ऐसे मामलों में भारत चाह कर बहुत कुछ नहीं कर सकता.
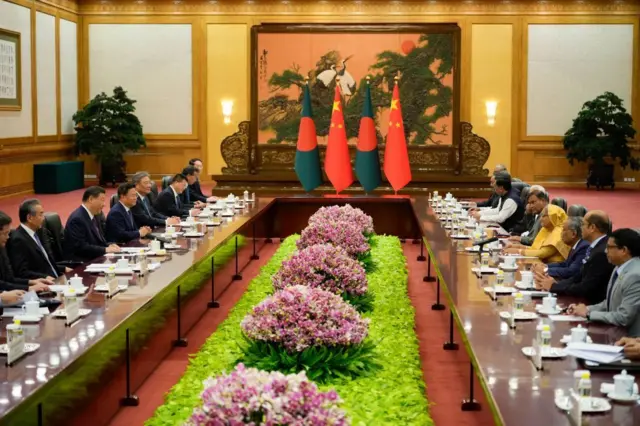
इमेज स्रोत, Getty Images
पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने कार्यकाल के दौरान कहा था कि हम सब कुछ बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसियों को नहीं बदल सकते. हमें इस भूगोल के साथ ही चलना होगा.
यह बात भारत के पड़ोसियों के मामले में भी सच है. भारत जहां है, वहीं रहेगा, वह लोग चाह कर भी भारत को खुद से दूर नहीं कर सकते.
इसलिए यह जिम्मेदारी पारस्परिक है. संबंध बिगड़ने के लिए किसी एक देश की नीति की गलती को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, इसके लिए दोनों देश जिम्मेदार होते हैं. जब दोनों के हित मिलते हैं तो संबंध सहज रहते हैं और इनमें टकराव होने पर पग-पग पर ठोकर लगती है.
विभिन्न देशों में भारत के खिलाफ असंतोष क्यों पनप रहा है? इस सवाल के जवाब मैं कहूंगा कि इसमें व्यावहारिक कारक के अलावा संरचनात्मक कारक भी शामिल हैं.
बांग्लादेश एक मुस्लिम बहुल देश है. भारत में मुस्लिमों पर अत्याचार की किसी घटना से वहां असंतोष पनप सकता है, यह व्यावहारिक कारक है.
इसके अलावा इस क्षेत्र में भारत की संरचनात्मक विषमता के कारण पड़ोसी देश उसे एक आधिपत्य शक्ति के तौर पर देखते हैं.
उन देशों में कुछ ताकतें अपने हित में भारत-विरोध भावना को हवा देते हैं, इसे संरचनात्मक कारक कहा जा सकता है.
इसमें कुछ नया नहीं है. यह लंबे समय से चल रहा है और आगे भी रहेगा.
लेकिन मुझे लगता है कि किसी पड़ोसी देश में भारत के ख़िलाफ़ नाराज़गी के सिर उठाने के लिए भारत की विदेश नीति में गलती तलाशना उचित नहीं होगा.
(बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए आप यहां क्लिक कर सकते हैं. आप हमें फ़ेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं.)