क्यों भूल जाते हैं हम बचपन की बातें?
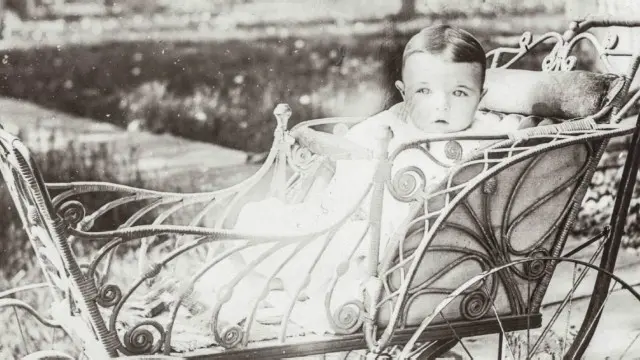
इमेज स्रोत, simpleInsomnia Flickr CCBY2.0
- Author, ज़ारिया गॉर्वेट
- पदनाम, बीबीसी फ़्यूचर
हम बचपन में बहुत से लोगों से मिलते हैं. उनके साथ वक़्त बिताते हैं. खाते-पीते हैं. पार्टी करते हैं. घूमने-फिरने जाते हैं.
बहुत से लोगों के साथ बचपन का अच्छा-ख़ासा वक़्त बिताने के बावजूद हमें उस वक़्त की कोई बात याद नहीं रहती है.
कभी आपने सोचा है कि पैदा होने के बाद के कुछ साल हमें क्यों याद नहीं रहते?
बरसों से मां-बाप, मनोवैज्ञानिक, न्यूरोसाइंटिस्ट और ज़बान के जानकार इस पहेली का हल तलाशने की कोशिश कर रहे हैं.
मशहूर मनोवैज्ञानिक सिग्मंड फ्रायड ने बचपन की बातों के याद न होने की इस पहेली को 'इन्फैंट एम्नेज़िया' नाम दिया था.
मतलब, बचपन का भुल्लकड़पना.
बहुत से लोग अपने बचपन के क़िस्से यूं सुनाते हैं जैसे वो कल की ही बात हो.
लेकिन कुछ लोगों को छह-सात बरस की उम्र तक की कोई भी बात याद नहीं रहती.
जो लोग बड़े चाव से बचपन के क़िस्से सुनाते हैं, उनमें से कई क़िस्से तो हक़ीक़त होते ही नहीं.
वो सुनी-सुनाई बाते होती हैं, जिन्हें दिमाग़ याद के तौर पर सहेजकर रख लेता है.
लेकिन कभी-कभी बचपन की यादों का न होना इसलिए भी परेशान करता है क्योंकि यही उम्र होती है जब बच्चों का दिमाग़ तेज़ी से विकसित होता है.
बच्चों के दिमाग़ में हर सेकेंड 700 नई तंत्रिकाएं बनती हैं.
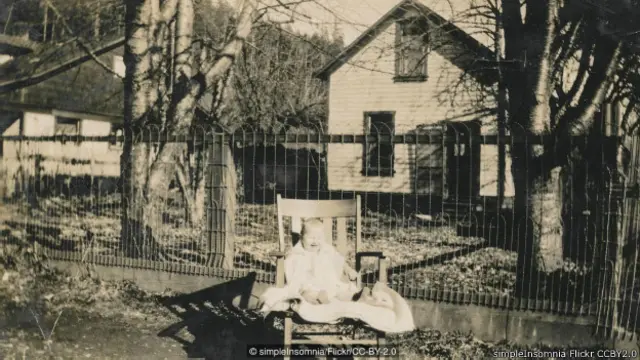
इमेज स्रोत, simpleInsomnia Flickr CCBY2.0
इनके ज़रिए वो बोलना सीखते हैं और ज़िंदगी का सलीका भी सीखते हैं.
रिसर्च बताते हैं कि बच्चे तो मां के पेट से ही सीखना शुरू कर देते हैं.
फिर भी वो बचपन की यादों को क्यों नहीं सहेज पाते?
असल में होता ये है कि हमारा दिमाग़ ख़ुद ही ये फ़ैसला कर लेता है कि कितनी बातें सहेजकर रखनी हैं और कितनी भुला देनी हैं.
तमाम तजुर्बे बताते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी की दो से तीन फ़ीसद बातें ही लंबे वक़्त तक याद रखते हैं. बाक़ी बातों को हमारा दिमाग़ भुला देता है.
उन्नीसवीं सदी में जर्मन मनोवैज्ञानिक हर्मन एबिंगहॉस ने ख़ुद पर एक तजुर्बा किया था.
और एक महीने बाद तो जो भी हर्मन ने सीखा था, उनके दिमाग़ में उसकी दो-तीन फ़ीसद याद ही बाक़ी बची थी.
ऐसा बच्चों के साथ भी होता है. ज़्यादातर बातें वो भूल जाते हैं. क्योंकि उनका दिमाग़ उन्हें ग़ैरज़रूरी समझकर फेंक देता है.
वैसे हमारे बचपन की याददाश्त का हमारे माहौल से सीधा ताल्लुक़ है.
जैसे कि चीन में बचपन की याद को ग़ैरज़रूरी माना जाता है.

इमेज स्रोत, simpleInsomnia Flickr CC BY 2.0
वहीं अमरीका में लोग बचपन के क़िस्से बढ़-चढ़कर बताते हैं.
ऐसे में अमरीकियों के पास बचपन की कुछ यादें होती हैं. वे तफ़्सील से उस बारे में बात करते हैं.
कई बार उसे बढ़ा-चढ़ाकर भी पेश करते हैं. वहीं चीनी सभ्यता में इसे अहमियत नहीं दी जाती.
इसलिए वहां के लोगों की बचपन की याददाश्त उतनी मज़बूत नहीं होती.
चीनी मूल की अमरीकी मनोवैज्ञानिक की वांग ने इस बारे में रिसर्च किया था.
उन्होंने सैकड़ों अमरीकी और चीनी छात्रों के बचपन की यादों के आंकड़े जमा किए.
उन्होंने पाया कि अमरीकी छात्रों को बचपन के क़िस्से पूरी तरह याद थे. वहीं चीनी छात्र इसमें कमज़ोर पाए गए.
कई बार अपने बारे में सोचना भी याददाश्त को सहेजने में मददगार होता है.
क्योंकि फिर आप हर घटना से ख़ुद को जोड़ लेते हैं. इस वजह से वो घटना, वो बात याद रह जाती है.
कुछ मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि बोलना आना, हमारी याददाश्त के लिए सबसे मददगार होता है.
जब बच्चे ज़बान सीखते हैं, तो उनके ख़्यालों को शब्द मिल जाते हैं.
फिर वो शब्द क़िस्सों में तब्दील हो जाते हैं. यही क़िस्से याददाश्त के तौर पर हमारा दिमाग़ सहेजकर रख लेता है.

इमेज स्रोत, Kimberly Hopkins Flickr CC By 2.0
हालांकि कुछ मनोवैज्ञानिक इससे इत्तेफ़ाक़ नहीं रखते.
वो कहते हैं कि गूंगे बहरे बच्चों को भी बचपन की बातें याद रहती हैं.
ऐसे लोग ब्रेल लिपि से पढ़ना लिखना नहीं भी सीखते, तो आगे चलकर अपनी यादें साझा कर पाते हैं.
इसलिए याददाश्त का बोलने-सीखने से कोई ताल्लुक़ नहीं.
वैज्ञानिक मानते हैं कि बच्चों का दिमाग़ इतना विकसित नहीं होता कि वो यादों को सहेजकर रखे.
हमारी यादें दिमाग़ के जिस हिस्से में रहती हैं, उसे वैज्ञानिक 'हिप्पोकैम्पस' कहते हैं.
बच्चों के दिमाग़ का ये हिस्सा बेहद कम विकसित होता है. तब इसमें नई तंत्रिकाओं का विकास होता रहता है.
जब 'हिप्पोकैम्पस' का विकास पूरी तरह से हो जाता है. उसके बाद से ही हमारा दिमाग़ यादों को सहेजकर रखने का काम शुरू करता है.
कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि 'हिप्पोकैम्पस' की ग़ैरमौजूदगी में भी यादों को हमारा दिमाग़ सहेजता रहता है.
मगर वो दिमाग़ के ऐसे हिस्से में जाकर बंद हो जाती हैं कि हम उन्हें फिर से निकाल नहीं पाते.
अभी वैज्ञानिकों को भी दिमाग़ की उस अलमारी की चाभी नहीं मिली, जहां बचपन की ये यादें बंद रहती हैं.

इमेज स्रोत, simpleInsomnia Flickr CC By 2.0
कई बार बचपन के कुछ झूठे क़िस्सों को भी हम अपनी यादों का हिस्सा बना लेते हैं.
कुछ लोग तो इन क़िस्सों में अपनी तरफ़ से भी नई बातें जोड़ लेते हैं और फिर उन्हें बढ़ा-चढ़ाकर पेश करते हैं.
अमरीका की कैलिफ़ोर्निया यूनिवर्सिटी की एलिज़ाबेथ लोफ्ट्स ने इस बारे में दिलचस्प तजुर्बा किया था.
उन्होंने कुछ बच्चों को झूठे क़िस्से गढ़कर सुनाए.
इसके बाद उनके मां-बाप से उन क़िस्सों की तस्दीक़ भी करा दी.
इसके बाद उन बच्चों ने उस झूठी घटना के बारे में बढ़-चढ़कर बताना शुरू कर दिया.
कुछ यूं जैसे उन्हें वो अच्छी तरह से याद हो. हालांकि वो घटना पूरी तरह से काल्पनिक थी.
वैसे भी सच्ची घटनाओं से जुड़ी हमारी यादें भी वक़्त के साथ नए रंग-रूप में हमारे सामने आती हैं.
हमारा दिमाग़ उनमें हेर-फेर कर डालता है.
ऐसा उन घटनाओं के बारे में अक्सर होता है जिनकी हमें ख़ुद याद नहीं, बल्कि किसी और से हमने उनके बारे में सुना होता है.
तो सवाल ये नहीं कि बचपन की बातें क्यों याद नहीं रहतीं. असल सवाल ये है कि क्या हम उन यादों पर यक़ीन कर सकते हैं?
(अंग्रेज़ी में मूल लेख पढ़ने के लिए <link type="page"><caption> यहां क्लिक करें</caption><url href="http://www.bbc.com/future/story/20160726-the-mystery-of-why-you-cant-remember-being-a-baby" platform="highweb"/></link>, जो <link type="page"><caption> बीबीसी फ्यूचर</caption><url href="http://www.bbc.com/future" platform="highweb"/></link> पर उपलब्ध है.)
(बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए आप <link type="page"><caption> यहां क्लिक कर</caption><url href="http://www.bbc.co.uk/hindi/multimedia/2013/03/130311_bbc_hindi_android_app_pn.shtml" platform="highweb"/></link> सकते हैं. आप हमें <link type="page"><caption> फ़ेसबुक</caption><url href="https://www.facebook.com/bbchindi" platform="highweb"/></link> और <link type="page"><caption> ट्विटर</caption><url href="https://twitter.com/BBCHindi" platform="highweb"/></link> पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं.)












