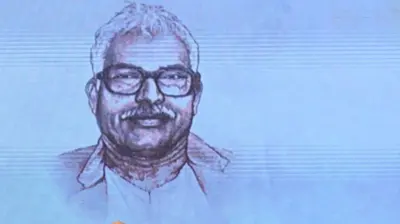सऊदी अरब जिस डर के कारण तमाम दबाव के बावजूद नहीं ले पा रहा फ़ैसला

इमेज स्रोत, Getty images
- Author, प्रियंका झा
- पदनाम, बीबीसी संवाददाता
बीते कुछ सालों में इसराइल और अरब देशों के बीच रिश्ते धीरे-धीरे पटरी पर लौटने शुरू हुए हैं.
संयुक्त अरब अमीरात (यूएई), बहरीन, सूडान और मोरक्को ने इसराइल के साथ अपने औपचारिक संबंधों की शुरुआत की है लेकिन मुस्लिम देशों के अगुवा माने जाने वाला सऊदी अरब अब भी रिश्तों को सामान्य करने से हिचकिचाता दिख रहा है.
अमेरिका की अगुवाई में सऊदी अरब और इसराइल के बीच शांति समझौते की अटकलें ज़रूर लगाई जा रही हैं, लेकिन सऊदी ने बीते सप्ताह फ़लस्तीन में नायेफ़ अल-सुदैरी को अपना राजदूत नियुक्त कर के ये साफ़ कर दिया है कि फ़िलहाल वो इसराइल के साथ रिश्ते आगे बढ़ाने पर जल्दबाज़ी करने के मूड में नहीं हैं.
इसराइल और फ़लस्तीन के बीच विवाद में अब तक सऊदी अरब खुलकर फ़लस्तीन का समर्थन करता आया है. सऊदी अरब और इसराइल के बीच राजनयिक संबंध नहीं है.
दोनों मुल्कों के बीच रिश्तों को लेकर चर्चा वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के बाद फिर से तेज़ हुई.
इस रिपोर्ट में दावा किया गया था कि अमेरिका ने सऊदी अरब के साथ उस समझौते की रूप-रेखा तैयार कर ली है, जिसके ज़रिए इसराइल और सऊदी के रिश्तों को सामान्य किया जाएगा.
रिपोर्ट में कुछ अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से ये आशा जताई गई कि अगले 9 से 12 महीने के अंदर मध्य पूर्व क्षेत्र में इस युग का सबसे अहम शांति समझौते पर बात बन सकती है.
ये भी दावा किया गया कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान (एमबीएस) ने अमेरिकी अधिकारियों को ये भरोसा दिलाया है कि वो 'समझौते पर पहुँचने की कोशिश को लेकर गंभीर हैं.
हालांकि, ख़बरें ये भी आईं कि दूसरी तरफ़ एमबीएस ने अपने क़रीबियों से कथित तौर पर कहा है कि वो इसराइल के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने के लिए तैयार नहीं हैं.
जानकार सऊदी अरब के इस अस्पष्ट रुख़ के पीछे कई कारण गिनाते हैं.
ऐसा माना जा रहा है कि अब तक फ़लस्तीन के मुद्दे को ज़ोर-शोर से उठाते आ रहे सऊदी अरब को इसराइल के साथ समझौता करने से घरेलू स्तर पर भारी बग़ावत झेलनी पड़ सकती है.
साथ ही इससे अंतरराष्ट्रीय समुदाय, ख़ासतौर पर मुस्लिम देशों के बीच सऊदी की नेता वाली स्थिति को भी बड़ा धक्का लग सकता है.
'ईरान फ़ैक्टर' की वजह से पसोपेश में सऊदी अरब

इमेज स्रोत, Getty Images
मध्य-पूर्व में दशकों से दुश्मन रहे सऊदी अरब और ईरान के रिश्ते ने इस साल बड़ा बदलाव देखा.
मार्च महीने में सऊदी अरब और ईरान के अधिकारियों के बीच चीन में चली चार दिन की बातचीत के बाद दोनों ने कूटनीतिक रिश्ते बहाल करने की अप्रत्याशित घोषणा हुई.
सऊदी अरब में एक जाने-माने शिया धर्म गुरु को फांसी दिए जाने के बाद रियाद स्थित सऊदी दूतावास में ईरानी प्रदर्शनकारी घुस आए थे.
2016 में इस घटना के बाद सऊदी अरब ने ईरान से अपने राजनयिक रिश्ते तोड़ लिए थे. इसके बाद से सुन्नी बहुल सऊदी अरब और शिया बहुल ईरान के बीच भारी तनाव रहा है.
मध्य-पूर्व में वर्चस्व की होड़ में लगे दोनों देश एक-दूसरे को अपने लिए ख़तरा मानते रहे हैं.
इसी वजह से दोनों देश लेबनान, सीरिया, इराक़ और यमन समेत मध्य-पूर्व के कई देशों में प्रतिद्वंद्वी गुटों को समर्थन देते रहे हैं.
हालांकि दोनों देशों का एक-दूसरे पर पूरी तरह भरोसा अभी तक नहीं बन सका है.
जानकार मानते हैं कि अगर सऊदी अरब इसराइल के साथ कूटनीतिक रिश्ते स्थापित करता है तो ईरान इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएगा.
साथ ही इससे सऊदी अरब की इस्लामिक देशों की अगुवा वाली स्थिति भी ख़तरे में आ जाएगी.
वो भी तब जब ईरान और दूसरे बड़े इस्लामिक देश मुस्लिम देशों की अगुवाई करने की इच्छा ज़ाहिर कर चुके हैं.
दिल्ली के जेएनयू विश्वविद्यालय में पश्चिम एशिया मामलों के अध्यापक प्रोफ़ेसर एके पाशा कहते हैं, "ईरान के सहयोगी हिज़बुल्लाह, हमास और हूती भी अपनी नाराज़गी जताएंगे. इसमें ईरान का पलड़ा भारी होगा क्योंकि फ़लस्तीन का मुद्दा इस्लामिक देशों के बीच 'भावनात्मक' मुद्दा है.''
''ये भी हो सकता है कि ईरान से जो रिश्ते सुधरे हैं, उसमें फिर से नाराज़गी बढ़े. इसलिए उन्होंने (सऊदी अरब) जॉर्डन में अपने मौजूदा राजनयिक को ही फ़लस्तीन के राजनयिक के तौर पर अतिरिक्त ज़िम्मेदारी सौंपी है, कोई नया राजनयिक नियुक्त नहीं किया है."
एके पाशा का ये भी कहना है कि जबसे बाइडन राष्ट्रपति बने हैं, तबसे मानवाधिकार सहित कई अन्य मुद्दों को लेकर सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ उनके रिश्ते अच्छे नहीं हैं.
प्रोफ़ेसर पाशा कहते हैं, "ऐसे में एमबीएस की इच्छा है कि अमेरिका उनकी सत्ता को सपोर्ट करे और वो अमेरिका के साथ डिफ़ेंस ट्रीटी करना चाहते हैं. दूसरा ये कि चीन के दख़ल से ईरान के साथ सऊदी अरब के कूटनीतिक रिश्ते सुधरे हैं लेकिन फिर भी सऊदी अरब ईरान को अपने लिए सैन्य और वैचारिक स्तर पर अपने लिए ख़तरा मानता है.''
''इसलिए सऊदी चाहता है कि अमेरिका उसे अच्छे और आधुनिक हथियार दे. सऊदी अरब ये भी चाहता है कि ईरान के न्यूक्लियर रिएक्टर के जवाब में उसे सिविल न्यूक्लियर रिएक्टर मिले. सऊदी ने यही तीन मांगें अमेरिका के सामने रखी हैं."
लेकिन ये इन तीनों समझौते हक़ीक़त बने इसके लिए अमेरिकी कांग्रेस में इसराइली लॉबी का मानना बहुत ज़रूरी है.
इस्लामिक देशों के बीच 'धार्मिक पहचान' को नुक़सान?

इमेज स्रोत, Getty Images
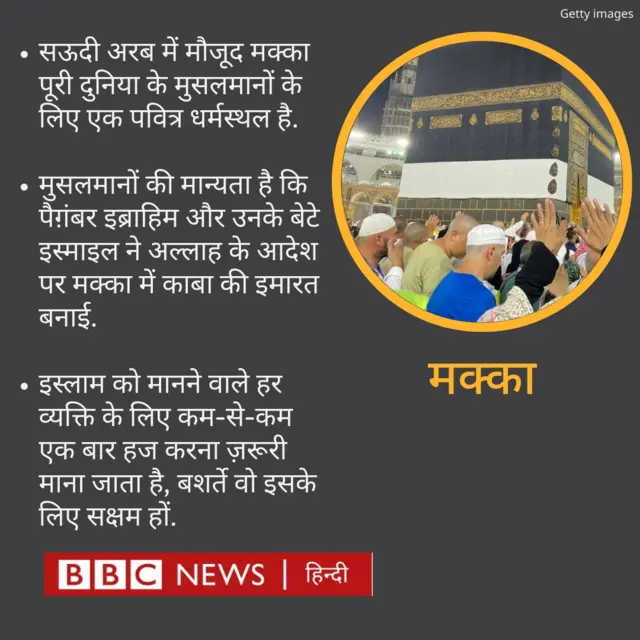
इमेज स्रोत, Getty Images
सऊदी अरब के पास मुसलमानों के दो सबसे पवित्र स्थल मक्का और मदीना हैं. लिहाजा यह ख़ुद को मुस्लिम दुनिया के नेता के रूप में देखता है.
इसके कारण मुस्लिम बहुल देशों के बीच सऊदी अरब की एक 'धार्मिक पहचान' है.
इस्लाम का तीसरा सबसे पवित्र स्थल अल-अक्सा मस्जिद इसराइल और फ़लस्तीन के बीच विवाद की जड़ यरुशलम में है. यहूदियों के लिए भी ये सबसे पवित्र जगह मानी जाती है.
सऊदी अरब कहता आया है कि जब तक फ़लस्तीन 1967 की सीमा के तहत एक स्वतंत्र मुल्क नहीं बन जाता है तब तक इसराइल से औपचारिक रिश्ता कायम नहीं करेगा. सऊदी अरब पूर्वी यरुशलम को फ़लस्तीन की राजधानी बनाने की भी मांग करता है.
अरब दुनिया और इसराइल के बीच की शत्रुता 1967 में छह दिनों के भीषण युद्ध के बाद से बढ़ गई थी.
इस युद्ध में इसराइल की जीत हुई थी. अरब देशों को एकजुट होकर भी हार का सामना करना पड़ा था.
इसराइल अपनी तरफ़ से ये आश्वासन देता रहा है कि शांति बहाली की राह में फ़लस्तीन 'अड़चन' नहीं होगा.
लेकिन विश्लेषकों की नज़र में अल-अक्सा पर इसराइल का रुख़ सामने होने के बावजूद अगर सऊदी अरब उसके साथ शांति समझौता करता है तो इससे इस्लामिक देशों के बीच उसकी छवि ख़राब होगी.
इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफ़ेयर के फ़ेलो और मध्य-पूर्व मामलों के जानकार फज़्ज़ुर रहमान सिद्दीक़ी कहते हैं, "सऊदी अरब की एक धार्मिक पहचान है. मुसलमानों के तीन में से दो पवित्र स्थल सऊदी अरब में हैं और वो उनके कस्टोडियन है. सऊदी अरब ने इतने सालों में फ़लस्तीन के मुद्दे को मुस्लिम वर्ल्ड का साझा मुद्दा बनाने में चैंपियन की भूमिका निभाई है. इसे इस्लामिक मुद्दा बताया गया, इसकी वजह ये भी है कि वहां (यरुशलम) पर मुसलमानों की तीसरा सबसे पवित्र धार्मिक स्थल (अल-अक्सा) है."

इमेज स्रोत, Getty Images
सिद्दीक़ी कहते हैं, "सऊदी अरब से इस्लामिक भावनाएं जुड़ी हैं. हर साल दुनियाभर के 25-30 लाख लोग मक्का-मदीना जाते हैं. इसलिए सऊदी अरब के लिए ये फ़ैसला (इसराइल से रिश्ते सामान्य करना) सबसे मुश्किल साबित होगा. उसे दुनिया भर के मुसलमानों का विरोध झेलना पड़ सकता है."
वह कहते हैं, "पहला तो मुस्लिम वर्ल्ड में सऊदी अरब का जो स्थान है, उसे बहुत बड़ा धक्का लगेगा. उसकी धार्मिक पहचान को बहुत नुक़सान पहुँचेगा. तीसरी बात ये है कि ईरान, तुर्की, पाकिस्तान, सऊदी अरब ऐसे देश हैं तो तकरीबन 50-60 साल से मुसलमानों के मुद्दों को लेकर आगे चलते हैं, उनके बीच अपनी धार्मिक पहचान की वजह से सऊदी अरब की जो रणनीतिक स्थिति है, वो उसे खो देगा."
एके पाशा की राय भी कुछ इसी से मिलती-जुलती है.
उनका कहना है,"सऊदी अरब इसराइल के साथ रिश्तों पर कोई ठोस फ़ैसला इसलिए नहीं ले पा रहा क्योंकि उसे चिंता है कि अगर इसराइल को मान्यता दे दी तो इस्लामिक देशों के संगठन (ओआईसी) जैसे अन्य गुटों के बीच उसकी क्या स्थिति होगी. वो ये भी नहीं जानता कि पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान या फिर इंडोनेशिया-तुर्की में, इस पर क्या प्रतिक्रिया देंगे."
फ़ज़्ज़ुर सिद्दीक़ी कहते हैं कि इसराइल के साथ रिश्ते बनाने का साफ़ अर्थ है कि आपने फ़लस्तीनी मुद्दे को पूरी तरह छोड़ दिया. वो कहते हैं कि ये सारे तथ्य सऊदी अरब को इसराइल के साथ रिश्तों को आगे बढ़ाने से रोक रहे हैं.
यूएई-मोरक्को कर सकते हैं तो सऊदी अरब क्यों नहीं?

इमेज स्रोत, Getty Images
साल 1979 में मिस्र ने इसराइल के साथ शांति समझौता किया था. ये समझौता व्हाइट हाउस में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर के सामने हुआ था.
इसके कई बरस बाद 1994 में जॉर्डन ने इसराइल के साथ पीस डील की. लेकिन फिर साल 2020 में एक लहर आई और बहरीन, यूएई, मोरक्को, सूडान जैसे मुस्लिम बहुल देशों ने इसराइल के साथ रिश्ते सामान्य करने के लिए 'अब्राहम अकॉर्ड' पर हस्ताक्षर किए थे. इसके बाद यूएई और बहरीन ने इसराइल के साथ राजनयिक रिश्ते भी कायम कर लिए थे.
लेकिन सऊदी अरब के लिए ये समझौता इतना मुश्किल क्यों है.
इस पर सऊदी अरब में भारत के राजनयिक रह चुके तलमीज़ अहमद कहते हैं, "इसराइल से रिश्ते बनाने वाले सिर्फ़ चार अरब देश हैं. सूडान खुद गृह युद्ध चल रहा है. उसकी गिनती ही नहीं है. जहाँ तक मोरक्को का सवाल है तो उसने सिर्फ़ दोनों देशों के बीच उड़ानें शुरू की है, लेकिन अपना राजनयिक नहीं भेजा है. सिर्फ़ यूएई ऐसा देश है जिसने थोड़ी पहल दिखाई है इसराइल से रिश्ते बनाने में. यूएई भी बहुत छोटा देश है और उसकी रणनीतिक अहमियत नहीं है."
वो कहते हैं कि सऊदी अरब के रास्ते में कई मुश्किले हैं, जिनमें सबसे पहला तो क़रीब 20 साल पहले हुआ अरब पीस इनिशिएटिव समझौता.

इमेज स्रोत, Getty Images
इस समझौते की पहल सऊदी अरब ने की थी और इसे अरब देशों ने स्वीकार किया था. इसका मक़सद था कि 1967 के बाद इसराइल ने जितने अरब क्षेत्रों पर कब्ज़ा किया है, वो वहाँ से पीछे हटे. साथ ही फ़लस्तीन को एक राष्ट्र के तौर पर मान्यता दे, जिसकी राजधानी पूर्वी यरुशलम होगी.
तलमीज़ अहमद कहते हैं, "इसराइल की ओर से भी फ़लस्तीन पर कोई डील पेश करनी चाहिए. बल्कि इसराइल की मौजूदा सरकार में तो ज़ुल्म और बढ़ गया है. ऐसे माहौल में ख़ुद को अरब वर्ल्ड और इस्लामिक लीडर समझने वाले सऊदी अरब के लिए आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है."
'द यरुशलम पोस्ट' के एक ओपिनियन आर्टिकल में भी इस सवाल का जवाब मिलता है.
इस लेख के अनुसार, यूएई की इच्छा अपने आपको मध्य-पूर्व और दक्षिण एशिया के कमर्शियल और फाइनेंशियल हब के तौर पर स्थापित करना है. यूएई ने अपने देश में काम के लिए रह रहे दक्षिण एशियाई मज़दूरों को ध्यान में रखते हुए मंदिर तक बनवाया है. लेकिन सऊदी की छवि धार्मिक है. यूएई की उदार नीतियों के विपरीत वो मुसलमानों के पवित्र स्थलों के रखवाले के तौर पर गौरव महसूस करता है.
डील का हासिल क्या?

इमेज स्रोत, Getty Images
इसराइल के सबसे बड़े रणनीतिक सहयोगी अमेरिका ने अरब दुनिया और इसराइल के बीच संबंध सुधारने की दिशा में पहल शुरू की थी.
मिस्र और जॉर्डन के साथ दशकों पहले हुए समझौता हो या फिर 2020 में हुआ अब्राहम अकॉर्ड. इन सभी मौकों पर तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति की भूमिका अहम रही.
सऊदी अरब और इसराइल के बीच समझौता करवाने की पहल जो बाइडन ने की है लेकिन अमेरिका को इस समझौते से क्या मिलेगा.
इस पर तलमीज़ अहमद कहते हैं, "अमेरिका में अगले साल राष्ट्रपति चुनाव होने हैं. अगर ये डील हो जाती है तो जो बाइडन के पास चुनाव में उतरने से पहले एक बड़ी कामयाबी होगी."
वहीं, एके पाशा की नज़र में भी इससे इसराइल को सबसे ज़्यादा फ़ायदा है. इसराइल की मौजूदा सरकार अपने ही घर में न्यायिक सुधारों के ख़िलाफ़ बड़े स्तर पर विरोध झेल रही है.
अगर ये समझौता होता है तो इसराइल को घरेलू संकट से ध्यान भटकाने में मदद होगी.
हालांकि, सऊदी अरब को इस सौदे से कुछ ठोस हासिल नहीं होने जा रहा है.
एके पाशा कहते हैं, "सऊदी अरब ये भी जानता है कि अगले साल अमेरिका में सत्ता बदली तो हो सकता है कि उसे मिलने वाली मदद पहले की तरह नहीं रहेगी. बल्कि इससे फ़ायदा इसराइल को होगा. वो अंतरराष्ट्रीय समुदाय के बीच ये कह पाएगा कि सबसे बड़े इस्लामिक देशों के नेता सऊदी अरब ने भी उसे स्वीकार्यता दे दी है."
"सऊदी अरब की सिर्फ़ आलोचना होगी और अंदरूनी कलह भी बढ़ सकती है. यहाँ तक कि शाही परिवार में भी फूट पड़ सकती है. पहले से ही परिवार के वरिष्ठ सदस्यों की गिरफ़्तारी, संपत्ति ज़ब्त करने जैसे कई कार्रवाइयों से मोहम्मद बिन सलमान के ख़िलाफ़ नाराज़गी का माहौल है. इसराइल को मान्यता देने से एमबीएस के विरोधियों को उन्हें घेरने का मौका मिल सकता है. ये फैसला एमबीएस की मुसीबतें बढ़ाने वाला साबित हो सकता है."
ये भी पढ़ें:
(बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए आप यहां क्लिक कर सकते हैं. आप हमें फ़ेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं.)