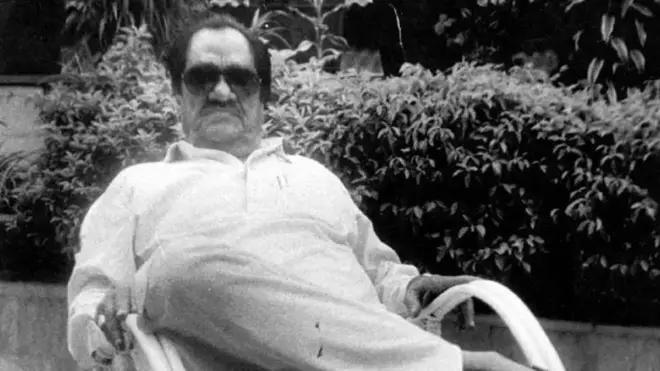अपनों के जाने पर मातम न कर पाने का दर्द

इमेज स्रोत, AFP
- Author, शिव विश्वनाथन
- पदनाम, समाजशास्त्री
मौत के इर्दगिर्द चाहे रहस्य का एक अजब सा घेरा हो, लेकिन मौत के बाद उपजे शोक से तालमेल बिठाने के दस्तूर हमेशा ही रहे हैं.
ये रस्में किसी अपने के बिछड़ने के बाद भी मायने भरी ज़िंदगी जीने में मदद करती हैं.
हरेक परिवार में किसी की मौत के बाद पारंपरिक रस्में निभाई जाती है.
किसी की दुनिया से विदाई भले ही निजी नुक़सान हो लेकिन मातम के दस्तूर के जरिए मौत का सामाजिक पहलू उभरकर सामने आता है.
शोक की रस्में

इमेज स्रोत, EPA
मौत के बाद शोक जताने की नाटकीय रस्मों के पीछे साफ और सामान्य से तर्क हैं.
जब किसी की मौत होती है तो उसका परिवार और रिश्तेदार शोक मनाते हैं.
उस दौर में खाना बनाने जैसे रोज़मर्रा के काम बंद हो जाते हैं. मौत का दुख, बिछड़ने वाले की कमी का अहसास, मातमी सूरत दिखती हैं और रोना-धोना शुरु हो जाता है.
लगभग हर समाज में मातम की कुछ रस्में हैं और उनका वक़्त भी मुक़र्रर है.
शोक मनाने के तरीके अलग-अलग हैं. कई समुदायों में रोने और शोक ज़ाहिर करने का काम परिवार के इतर पेशेवर लोग भी करते हैं जो मातम का दिखावा करते हैं.
इसके ज़रिए ऐसा ग़मगीन माहौल तैयार हो जाता है, जिसकी उम्मीद किसी की मौत के बाद की जाती है.
समझदारी

इमेज स्रोत, AP
मौत के बाद सार्वजनिक तौर पर रोने और शोक ज़ाहिर करने की परंपरा सी रही है.
शोक के दिन पूरे होने के बाद ज़िंदगी फिर ढर्रे पर लौट आती है.
ऐसी परंपराओं और शोक जाहिर करने के विधान के पीछे एक समझदारी दिखती है.
असल में जो लोग शोक के लिए तयशुदा वक़्त से ज़्यादा समय तक मातमी सूरत बनाए रहते हैं, उन्हें दिखावा करने वाला भी माना जाता है.
मौत और उसके बाद सार्वजनिक तौर पर मनाए जाने वाले शोक में सही संतुलन की उम्मीद की जाती है.
मुश्किल

इमेज स्रोत, Raajkumar Keswani
आज मौत की वजहे बदल गई हैं. आपदा, दंगे, महामारी, नरसंहार के वक्त रस्मी तौर पर दुख ज़ाहिर करना मुश्किल होता है.
भोपाल में हुई त्रासदी या फिर 1999 में ओडीशा में आए चक्रवात के वक़्त शवों की पहचान करनी मुश्किल हो गई और मृत्यु एक सामूहिक घटना बन गई.
मरने वालों के परिजन रस्मी तौर पर शोक न मना पाने की वज़ह से अवसाद में डूब गए थे. जब रस्मी मातम नहीं हो पाता तब दुख अंतहीन हो जाता है.
बिछड़ने वाले की कमी और ग़म ऐसे घाव बन जाते हैं, जिन्हें भरने के लिए रस्मों की जादुई दवा नहीं मिल पाती.
अनकही खामोशी खोने की पीड़ा को बढ़ा देती है और मानस पर भी चोट करती है.
आज के दौर में चरमपंथी घटनाओं या फिर बड़े हादसों की वजह से हुई मौतों के बाद मातम का रस्मी अंदाज नहीं दिखता.
अफ़सोस

इमेज स्रोत, AP
मुझे याद है कि ओडीशा के चक्रवात के बाद इस पर अध्ययन करने वाले पॉलिटिकल साइंटिस्ट चंद्रिका परमार को लोगों ने बताया था कि रस्में निभाना मुमकिन नहीं था.
उन्हें भोजन, दवाओं या फिर छत की कमी का शिकवा नहीं था, बल्कि अफ़सोस यह था कि वो मरने वाले के अंतिम संस्कार भी पूरे नहीं कर सके.
शोक के सिलसिले को ख़त्म करने के लिए आरएसएस और आनंद मार्ग जैसे संगठनों ने सामूहिक रस्में निभाईं.
चरमपंथी घटनाओं के वक़्त भी ऐसी ही दिक्कतें सामने आती हैं. लाशें सही स्थिति में नहीं रहती हैं.
उनकी पहचान करना मुश्किल हो जाता है. मौत को लेकर रस्मी शोक की अदायगी नहीं हो पाती.
जैसा कि एक बार एक पीड़ित परिवार ने कहा था कि ये बदले की बात नहीं, बल्कि हम ग़म से उबरना चाहते हैं और ऐसा तभी हो सकता है जबकि जिंदगी के मायने हों.
आज की ज़िंदगी में ये बात सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक हो चुकी है.
चरमपंथ, नरसंहार और महामारी की बार-बार होने वाली घटनाओं के बीच मौत असहाय हो गई है, क्योंकि समाज मातम नहीं कर पाता है.
मातम न कर पाने से ऐसा जहनी ज़ख़्म बन जाता है, जिसे समाज को झेलना पड़ता है और जिसका उसके पास कोई सही जवाब भी नहीं है.
प्रेत छाया

इमेज स्रोत, Getty
साल 1967 में जर्मन मनोवैज्ञानिक अलेक्जेंडर और मार्गरेट मिस्चेरलिच ने मातम न कर पाने पर एक अहम किताब लिखी.
मस्चेरलिच ने मातम और गहरी उदासी के बीच अंतर बताते हुए लिखा कि जर्मनी के लोगों ने हिटलर से लंबे समय तक रहे अपने जुड़ाव को सही तरीके से ख़त्म किए बग़ैर ही युद्ध के बाद के के नए दौर से ख़ुद को जोड़ लिया.
जर्मनी के लोगों ने भूलने और नकारने का सिस्टम विकसित कर लिया और कभी अतीत से छुटकारा पाने की कोशिश नहीं की.
इसका नतीजा यह हुआ कि जर्मनी के लोगों का मानस कभी हिटलर के प्रेत से मुक्त नहीं हुआ. इसकी वज़ह यह है कि वे इससे छुटकारा पाने के लिए ज़रूरी रस्मों से नहीं गुजरे.
नतीजतन, उस दौर को उम्दा तरीके से याद करने के बजाए उस दौर की यादों से कड़वाहट पैदा होने की आशंका बनी रहती है.
त्रासदी

इमेज स्रोत, AFP
अंत में यह याद रखना होगा कि मौत को लेकर आधुनिक समाज का सामूहिक मानस बन जाता है.
टीवी के दर्शकों के तौर पर हम दूसरों के लिए रोने वाले रुदाली बन गए हैं.
टीवी में चैनल बदलने का विकल्प होता है. इसके बावजूद आपदा की घटना का असर यह होता है कि उसे देखने वाला हिंसा देखकर निढाल हो जाता है, और अमूर्तता की स्थिति रोने धोने का मौका नहीं देती.
टीवी के ज़रिए रुदाली बने लोगों के पास उन भावनाओं से गुजरने और घटना पर प्रतिक्रिया देने का वक़्त नहीं होता. वे महज भौंडेपन के तमाशबीन बनकर रह जाते हैं.
यही वजह है कि देखने वाला ख़ून का प्यासा हो जाता है और वास्तविक पीड़ित के उलट बदला लेने की मांग करता है.
ख़ून का बदला ख़ून की मांग होने से दुनिया मातम ज़ाहिर करने की ताकत खोती जा रही है. यह बीसवीं शताब्दी की त्रासदी हो सकती है.
<bold>(बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए <link type="page"><caption> यहां क्लिक </caption><url href="https://play.google.com/store/apps/details?id=uk.co.bbc.hindi" platform="highweb"/></link>करें. आप हमें <link type="page"><caption> फ़ेसबुक</caption><url href="https://www.facebook.com/bbchindi" platform="highweb"/></link> और <link type="page"><caption> ट्विटर</caption><url href="https://twitter.com/BBCHindi" platform="highweb"/></link> पर भी फ़ॉलो कर सकते हैं.)</bold>