किसान आंदोलन मज़बूत मोदी सरकार के लिए सख़्त संदेश- नज़रिया
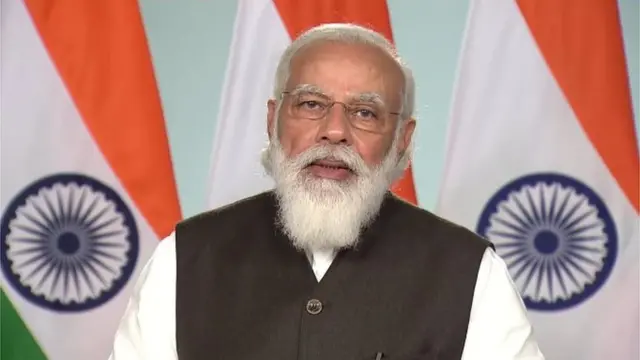
इमेज स्रोत, BJP
- Author, शिव विश्वनाथन
- पदनाम, समाजशास्त्री, बीबीसी हिंदी के लिए
समाज का ग़ैर-सरकारी और अराजनीतिक नेतृत्व जिसे लोग सिविल सोसाइटी भी कहते हैं, उसका बीच में ग़ायब हो जाना और दोबारा उभरकर सामने आना एक दिलचस्प बात है.
इस समय देश में जो कुछ चल रहा है उसमें सिविल सोसाइटी का उभार ऐसी बात है जो मोदी सरकार को ज़रूर चिंता में डाल रहा होगा.
जब पहली बार दिल्ली की सत्ता पर मोदी सरकार बैठी थी तो इसका राजनीतिक संदेश साफ़ था.
सरकार का लक्ष्य स्पष्ट था कि क्या करना है और क्या नहीं. इस शासन का दावा था कि जो देश की बड़ी आबादी के हित की बात होगी, वो उसी को आगे बढ़ाएँगे.

इमेज स्रोत, EPA
इस तरह सरकार ने ऐसा नागरिक समाज गढ़ लिया, जो सत्ता का ही एक्सटेंशन काउंटर था. यह एक ऐसी मशीन थी, जो 'देशभक्ति' जैसी आम सहमति वाली अवधारणाओं को मज़बूत करने में लगी थी.
'एंटी नेशनल' शब्द का लगातार इस्तेमाल इतना बढ़ा कि लोगों के विचारों की निगरानी जैसा माहौल बन गया, एक ऐसा माहौल जो सत्ता से मिलती-जुलती सोच कायम करने का दबाव बनाने लगा.
इस शासन के पहले कुछ सालों में सिविल सोसाइटी की पारंपरिक विविधता तो मानो ग़ायब होती दिख रही थी.
वर्चस्ववाद की यह कोशिश दो क़दमों से मज़बूत हुई. पहला, सभी ग़ैर-सरकारी संगठनों यानी एनजीओ को नौकरशाही की सख़्त निगरानी के दायरे में ले आया गया.
इस लेख में Google YouTube से मिली सामग्री शामिल है. कुछ भी लोड होने से पहले हम आपकी इजाज़त मांगते हैं क्योंकि उनमें कुकीज़ और दूसरी तकनीकों का इस्तेमाल किया गया हो सकता है. आप स्वीकार करने से पहले Google YouTube cookie policy और को पढ़ना चाहेंगे. इस सामग्री को देखने के लिए 'अनुमति देंऔर जारी रखें' को चुनें.
पोस्ट YouTube समाप्त, 1
दूसरा क़दम यह था कि अगर कोई शासन से असहमत है तो वह देश की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा के लिहाज से एक अवांछित तत्व है.
वरवर राव, सुधा भारद्वाज और स्टेन स्वामी जैसे मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को अर्बन नक्सल के जिन आरोपों के तहत गिरफ़्तार किया गया है और जिस तरह से इन मामलों की सुनवाई चल रही है, उस पर भी सवाल उठे हैं.
हुकूमत की यह जकड़बंदी बहुसंख्यकवाद के तौर पर सामने आई. यह बहुसंख्यक वर्चस्ववाद और उसके शीर्ष नेता के मज़बूत होने का संकेत था.
इसने यह भी संकेत दिया कि सरकार पर किसी तरह की प्रतिकूल टिप्पणी कर सकने वाले संस्थान मोटे तौर पर या तो सत्ता के सामने झुक जाएंगे या फिर महत्वहीन बना दिए जाएंगे.
ऐसा माहौल तैयार हुआ कि देश की सुरक्षा को भारी ख़तरा है और देश को बचाना सबसे पहली प्राथमिकता है. कोरोना वायरस संक्रमण ने इस तरह की हुकूमत को और हवा दी.
दरअसल, सिविल सोसाइटी के दोबारा उठ खड़े होने को पिछले कुछ समय में उभरे नीतिगत मुद्दों से जुड़ी घटनाओं की कड़ी के ज़रिये आंका जा सकता है. इनमें से हरेक घटना ने सिविल सोसाइटी के भविष्य और भाग्य पर अहम सवाल उठाए.
पहली घटना थी असम में नेशनल रजिस्टर पॉलिसी लागू करने की कोशिश.
भारतीय समाज की बाड़ाबंदी की गई और नागरिकता हासिल करना एक ऐसा संदिग्ध काम बन गया जो फ़र्ज़ी सर्टिफिकेट के सहारे पूरा हो सकता था. यह काम होना या न होना किसी क्लर्क की सनक पर टिका था.
एनआरसी के ख़िलाफ़ जो विरोध उठ खड़ा हुआ वो निश्चित तौर पर बीजेपी के बहुसंख्यकवाद के विस्तार का विरोध था. हालांकि सिविल सोसाइटी ने वह रास्ता खोज लिया था, जिसके सहारे वह असहमति ज़ाहिर करने में सक्षम होने लगा था.

इमेज स्रोत, Burhaan Kinu/Hindustan Times via Getty Images
शाहीन बाग़ और सिविल सोसाइटी का उभार
दिल्ली के जामिया मिलिया इलाक़े में मुस्लिम गृहिणियों के एक छोटा-सा विरोध प्रदर्शन एक बड़ी घटना बन गया.
इस प्रदर्शन में युगांतकारी घटनाओं के तत्व थे. सत्ता की ताक़त के ख़िलाफ़ किए गए नानियों-दादियों के इस प्रदर्शन ने दुनिया भर का ध्यान खींचा.
इस विरोध में एक सौम्यता थी और सादगी भी. उन गृहिणियों ने दिखाया कि वे संविधान की भावना को समझती हैं. उनमें एक समुदाय के तौर पर नागरिकता की समझ साफ़ दिख रही थी.
उन महिलाओं ने जो संदेश दिया और गांधी से लेकर भगत सिंह और आंबेडकर तक जिन विभूतियों की तस्वीरें उन्होंने उठा रखी थी, उसने देश के सामने लोकतंत्र का एक उत्सव ला दिया.

इससे भी ज़्यादा इसने यह दिखाया कि कैसे नागरिक समाज बगैर किसी राजनीतिक पार्टी और ट्रेड यूनियन के उभर आया है. एक कम्युनिटी नेटवर्क, एक राजनीतिक कल्पना- सिविल सोसाइटी की कल्पना को खिलने के लिए इसी बीज की तो ज़रूरत थी.
शाहीन बाग़ अपने मूल में एक सत्याग्रही आंदोलन था. एक राजनैतिक इनोवेशन था.
दरअसल, लोकतंत्र पर न तो राजनीतिक कार्यकर्ताओं का पेटेंट है और न कॉपीराइट. सड़कें ही डेमोक्रेसी का असल रंगमंच हैं और मानव शरीर ही विरोध का औजार.
वास्तव में उन महिलाओं ने ही अपने जवाब में यह ज़ाहिर कर दिया कि सिविल सोसाइटी को संविधान के आदर्शों पर सत्ता से अधिक भरोसा है.
इसने यह भी बताया कि लोकतंत्र कोई चुनावी परिघटना नहीं है. अगर इसे जीवंत बनाए रखना है तो प्रयोगों और सिविल सोसाइटी के रस्मों-रिवाज को बरकरार रखना होगा. सिविल सोसाइटी एक थियेटर की तरह लोकतंत्र की कल्पना को ज़िंदा रखती है.

इमेज स्रोत, Hindustan Times
हालांकि यहां कुछ एहतियात की ज़रूरत है. कोविड की वजह से एक विरोध स्थल के तौर पर शाहीन बाग़ का डेरा अब उठाया जा चुका है. यह पहले से ही एक तरह का मिथक बन चुका था.
कंपनियों के लिए निगरानी बड़ी सम्मोहक चीज़ होती है. सीएए ने जो डिज़िटल स्ट्रैटिजी पेश की थी वह कोविड संकट से और मज़बूत ही हुई है. सुरक्षा को सर्वोच्च रणनीति के तौर पर इस तरह पेश किया गया ताकि निगरानी लोगों को प्यार की तरह लगे.
सिविल सोसाइटी को ऐसी निगरानियों के प्रति सचेत रहना होगा. जीवन में लगातार बढ़ रही निगरानी टेक्नोलॉजी का प्रतिकार करने का ढंग खोजना होगा. असहमत पेशेवरों की भूमिका अब काफ़ी अहम हो गई है.
भारत के पास विरोध करने वालों का शाहीन बाग़ है लेकिन इसे असहमति की आवाज़ वाले पेशेवरों की भी ज़रूरत है. हमें एडवर्ड स्नोडन और जूलियन असांज जैसे लोगों की ज़रूरत है. वरना डिज़िटल महत्वाकांक्षाओं से भरे मध्यवर्ग को शायद यह अहसास ही न हो कि हमारे इर्द-गिर्द एक पूरा निगरानी तंत्र खड़ा हो गया है.

अगर सीएए से यह ज़ाहिर हुआ कि नागरिकता की परिभाषा का विचार संदिग्ध था तो कोविड और किसानों के विरोध प्रदर्शनों से यह साफ़ हुआ कि सुरक्षा और विकास के नाम पर उठाए गए क़दमों ने लोगों की आजीविका को ख़तरे में डाल दिया है.
किसानों के संघर्ष पर शुरुआती प्रतिक्रियाएं घिसीपिटी थीं. इन प्रदर्शनों को राष्ट्र विरोधी और नक्सलियों का आंदोलन कहा गया. एक बार फिर सिविल सोसाइटी ने किसानों के संघर्ष पर ध्यान दिया और इसे अपने फोकस में रखा.
लोगों ने महसूस किया कि मीडिया, ख़ास कर टीवी मीडिया किसानों के आंदोलन को नज़रअंदाज़ करने और उसकी छवि ख़राब करने मे लगा है.
कई टीवी चैनलों ने इसे मोदी के ख़िलाफ़ बग़ावत के तौर पर देखा है. इस सचाई को समझने की कोशिश नहीं की जा रही थी कि सरकार के सामने लोग अपनी रोज़ी रोटी के सवाल उठा रहे हैं.
असहमत नागरिक समाज ने इन ख़तरों से टकराना शुरू कर दिया है. हैदराबाद के नज़दीक चिराला बुनकरों का आंदोलन विकेंद्रित नेटवर्कों की मांग कर रहा है.
लेकिन सिविल सोसाइटी को सिर्फ़ अधिकारों के प्रति ही नहीं, समाज के प्रति भी संवेदनशील होना होगा. किसानों का आंदोलन सिर्फ़ बड़े किसानों की आवाज़ बन कर सीमित नहीं रह सकता. इसे सीमांत किसानों और भूमिहीन मज़दूरों की आवाज़ भी बनना होगा.
सिविल सोसाइटी को इनके बीच बोलना होता है और अलग-अलग आवाज़ों को सुन कर निर्णय भी करना होता है. इसे यह भी दिखाना है कि सत्ता के बड़े फ़ैसलों पर कैसे बहस चलानी है.
इस अर्थ में सिविल सोसाइटी को नई नॉलेज सोसाइटी बनना होगा और इसे भारतीय विविधता का ट्रस्टी भी होना होगा.
इन रुझानों को देखते हुए अब यह साफ़ हो गया है कि लोकतंत्र अब सिर्फ़ चुनावी परिघटना नहीं रह गया है और न ही अब यह पार्टियों तक सीमित है.
विपक्षी पार्टियां अब गूंगी या असरहीन दिखने लगी हैं, ऐसे में सिविल सोसाइटी को लोकतंत्र में नए प्रयोग करने होंगे. इसे अपना यह प्रयोग जड़ नहीं बल्कि अपने चेतन बुद्धिजीवियों के साथ मिलकर करना चाहिए.
इस लेख में Google YouTube से मिली सामग्री शामिल है. कुछ भी लोड होने से पहले हम आपकी इजाज़त मांगते हैं क्योंकि उनमें कुकीज़ और दूसरी तकनीकों का इस्तेमाल किया गया हो सकता है. आप स्वीकार करने से पहले Google YouTube cookie policy और को पढ़ना चाहेंगे. इस सामग्री को देखने के लिए 'अनुमति देंऔर जारी रखें' को चुनें.
पोस्ट YouTube समाप्त, 2
सिविल सोसाइटी की गतिशीलता के विपरीत ज़्यादातर विपक्षी पार्टियां अब लड़खड़ाती दिखती हैं. कांग्रेस लगातार घिसती हुई दिख रही है और वामपंथी एक क्लब या किसी एलीट सोसाइटी की तरह लगते हैं.
सिविल सोसाइटी को पार्टियों की स्थानीयता के अलावा देशीय और वैश्विक मुद्दों के इर्द-गिर्द नए सिरे से एकजुट होना होगा.
सुरक्षा के ढाल से लैस सत्ता, उसके निगरानी तंत्र और कॉर्पोरेट बाज़ारवाद से लड़ना अब आसान काम नहीं रह गया है.
( लेखक जाने माने समाजशास्त्री हैं और इन दिनों ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, सोनीपत के सेंटर फॉर नॉलेज सिस्टम के डायरेक्टर हैं. आलेख में उनके निजी विचार हैं)

(बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए आप यहां क्लिक कर सकते हैं. आप हमें फ़ेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं.)















