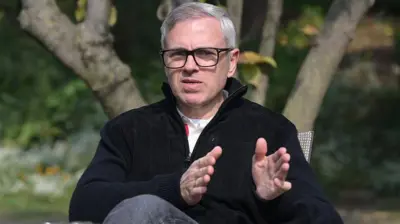दहेज़ हत्या की ख़बरें क्यों नहीं दिखतीं?

- Author, आकार पटेल
- पदनाम, वरिष्ठ विश्लेषक, बीबीसी हिन्दी डॉट कॉम के लिए
इस लेख को पढ़ने वाले बुज़ुर्गों को याद होगा कि आज से क़रीब 20 साल पहले अख़बारों में अक्सर दहेज़ हत्या की ख़बरें पढ़ने को मिलती थीं.
ये ख़बरें क़रीब एक जैसी ही होती थीं. हर दूसरे या तीसरे दिन अख़बार के पहले पन्ने पर दहेज़ हत्या की एक ख़बर मिलती थी, जिसमें किसी जवान औरत को आग के हवाले कर दिया गया हो और ससुराल वाले कहते थे कि रसोईघर में स्टोव फट गया. इन मामलों में ससुराल वाले और पति की गिरफ़्तारी हो जाती थी.
लेकिन ऐसी ख़बरें अब हमारे अख़बारों में नहीं आती हैं, ख़ासकर अंग्रेज़ी के अख़बारों में. ये ख़बरें टीवी पर तो बिल्कुल नहीं दिखाई जाती हैं, आख़िर क्यों?

इमेज स्रोत, MANISH SHANDILYA
इस दौरान कुछ क़ानून बनाए गए, जिसने ऐसी मौतों के बाद बेगुनाही का सुबूत देने की ज़िम्मेदारी ससुराल वालों पर सौंप दी है. अगर किसी महिला की मौत आग में जलने की वजह से हुई हो तो, आमतौर पर ऐसी मौत के बाद ससुराल वालों पर हत्या का आरोप ख़ुद ही लग जाता है.
तो क्या ऐसे कड़े क़ानूनों की वजह से ही हमें दहेज़ हत्या से जुड़ी ख़बरें पढ़ने को नहीं मिलती हैं, पर असल में इसके पीछे कुछ और ही वजह है.
हक़ीक़त यही है कि दहेज़ हत्या के मामले कम नहीं हुए हैं. वो इस दौरान भी बहुत ज़्यादा रहे हैं. साल 2015 में ऐसी 7634, 2014 में 8455, 2013 में 8083 और साल 2012 में 8233 मौतें हुई हैं.
भारत में हर रोज़ ऐसी हत्याओं के 20 से ज़्यादा मामले होते हैं. अगर ऐसी घटनाओं के आंकड़े 20 साल पहले से भी ज़्यादा हैं, तो हम अब उनके बारे में क्यों नहीं सुनते हैं?

इमेज स्रोत, REUTERS
दरअसल यह मीडिया की वजह है. ख़ासकर राष्ट्रीय और अंग्रेज़ी मीडिया की वजह से, जो अब ऐसी ख़बरों को रिपोर्ट ही नहीं करते हैं. आर्थिक लाभ न दे पाने वाली, अपराध या इंसानी सरोकार से जुड़ी ख़बरों में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है. मीडिया कवरेज में जानबूझ कर भारत की सबसे बड़ी आबादी को नज़रअंदाज़ किया जा रहा है.
अख़बार के मालिक और विज्ञापन से जुड़े लोग मानते हैं कि ऐसी ख़बरे या सीधे शब्दों में ऐसे लोग 'डाउन मार्केट' हैं. यानी कि बाज़ार के लिहाज से उनका कोई महत्व नहीं है.
इसके पीछे वजह बताई जाती है कि अंग्रेज़ी के पाठक ऐसी ख़बरों मे दिलचस्पी नहीं लेते हैं और वो 'अप मार्केट' ख़बरों को ज़्यादा पसंद करते हैं. मतलब कि पाठक अप मार्केट ख़बरों या अमीर और मशहूर लोगों में दिलचस्पी रखते हैं.

जब पहली बार साल 1995 के आस-पास यह सब शुरू हुआ, तो संपादकों और पत्रकारों ने इसका कुछ विरोध किया. लेकिन जैसा कि दहेज़ हत्या से जुड़ी ख़बरों के साथ हुआ, उन पत्रकारों को भी दबा दिया गया.
उसके बाद ऐसी घटनाओं की रिपोर्टिंग महत्व के आधार पर नहीं, बल्कि इनमें शामिल लोगों के आधार पर होने लगी.
मुंबई में ऐसे ही कुछ लोगों को ध्यान में रखकर पत्रकारिता शुरू हुई, जिसे उस वक़्त 'पेज-3' कहा जाता था. भूगोल या लोगों के बसावट के आधार पर ऐसी रिपोर्टिंग को आसान बनाया गया.

अख़बारों ने शहर के कुछ इलाक़ों, जिनमें मध्य वर्ग के या ग़रीब लोग रहते हों, वहां की ख़बरों को छापना बंद कर दिया. उनकी नज़र केवल उन इलाकों पर होती थी, जहां रईस और मशहूर लोग रहते थे.
मुझे कहना चाहिए कि कुछ हद तक इसने गैर अंग्रेज़ी अख़बारों पर भी असर डाला. एक दशक पहले जब मैं अहमदाबाद में एक गुजराती अख़बार का संपादक था तो ऐसा ही चल रहा था. उस वक़्त शहर के एक हिस्से की अनदेखी की जाती थी, क्योंकि उन इलाक़ों को मूल पाठकों का घर नहीं माना जाता था.
ये बातें पाठकों को दिलचस्प लग सकती हैं कि ऐसा ही कुछ भारतीय सिनेमा में भी हुआ. क़रीब 30 साल पहले, बॉलीवुड सिनेमा में किसी हीरो का एक ग़रीब परिवार से होना, उसके लिए शर्म की बात नहीं थी.

इमेज स्रोत, madhu pal
अमिताभ बच्चन ने 1983 में 'कुली' फ़िल्म में एक कुली का रोल किया था. लेकिन आज यह नामुमकिन है कि एक हीरो, मज़दूर वर्ग का होगा.
साल 1996 में बॉलिवुड में 'दिलवाले दुल्हनियां ले जाएंगे' और कुछ ऐसी ही फ़िल्में रिलीज़ हुईं. इन फ़िल्मों में भारत से जुड़ा कोई मुद्दा नहीं था, बल्कि रईस परिवारों के संकुचित सामाजिक मुद्दे थे.
इन फ़िल्मों ने उस भारतीय समाज की सच्चाई को पूरी तरह से नज़रअंदाज़ किया, जहां इसे बनाया जा रहा था.
इसी दौरान भारत में मॉल्स में मल्टीप्लेक्स मूवी थिएटर बनना शुरू हो गया था. इनके टिकट की क़ीमत, आम सिनेमा हॉल के टिकट से दोगुनी या उससे ज़्यादा होती थी और इसने भारत की एक बड़ी आबादी को पीछे धकेल दिया, जो इसका ख़र्च नहीं उठा सकते थे.
हालांकि अन्याय और हिंसा की यह दास्तां बॉलीवुड की उन फ़िल्मों में जारी रहीं, जिन्हें हम बी- ग्रेड फ़िल्म कहते हैं. ऐसी फ़िल्मों में धर्मेन्द्र और मिथुन चक्रवर्ती जैसे हीरो हुआ करते थे.

इमेज स्रोत, pr
ये फ़िल्में मल्टीप्लेक्स में नहीं, बल्कि छोटे शहरों (बी-क्लास) के आम सिनेमाघरों में दिखाई जाती थीं. लेकिन अब ऐसी फ़िल्में भी नहीं बनाई जाती हैं.
हमारी पत्रकारिता और फ़िल्मों में एक तरह की समानता है. उन्होंने जानबूझ कर ज़्यादातर लोगों को बाहर कर दिया है. केवल इसलिए नहीं कि उनकी कहानी अख़बारों या फ़िल्मों के लिए महत्व नहीं रखतीं. बल्कि इसलिए, क्योंकि माना जाता है कि भारत की शहरी आबादी, ऊंची जाति और उच्च वर्ग के पाठकों और दर्शकों को इन चीज़ों की कोई परवाह नहीं है.
(बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए आप <link type="page"><caption> यहां क्लिक कर </caption><url href="http://www.bbc.co.uk/hindi/multimedia/2013/03/130311_bbc_hindi_android_app_pn.shtml" platform="highweb"/></link>सकते हैं. आप हमें <link type="page"><caption> फ़ेसबुक</caption><url href="https://www.facebook.com/bbchindi" platform="highweb"/></link> और <link type="page"><caption> ट्विटर </caption><url href="https://twitter.com/BBCHindi" platform="highweb"/></link>पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं.)