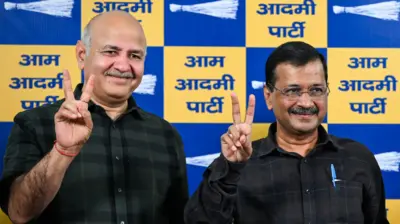हाथरस केस से फिर उठा सवाल, पुलिस सिस्टम में है जातिवाद?

इमेज स्रोत, HINDUSTAN TIMES/GETTY IMAGES
- Author, सर्वप्रिया सांगवान
- पदनाम, बीबीसी संवाददाता
पुलिस अधिकारी अपने जूनियर से पूछता है, 'एफआईआर क्यों नहीं लिखी अब तक?'
"सर केस इतना सीरियस लग नहीं रहा था"
"कब लगता है सीरियस?"
"इन लोगों के तो झूठे केस आते रहते हैं. अभी जनवरी में 'इनका' एक लड़का भाग गया था, इनके कहने पर किडनैपिंग का एफ़आईआर लिखा था सर, पूरे महीने 'इन लोगों' ने.."
पुलिस अधिकारी गुस्से में पूछता है, "किन लोगों ने?"
अफसर की डाँट सुनकर जूनियर पुलिसवाला सहम जाता है. लेकिन 'आर्टिकल-15' फ़िल्म का ये दृश्य कमज़ोर तबकों के साथ पुलिस के रवैये की चुगली कर जाता है.
समाज में जातिवाद का सच
ऐसे मामले सामने आते रहे हैं जहां किसी जातीय हिंसा में पुलिस ने पीड़ितों की रिपोर्ट दर्ज नहीं की, जांच में कोताही बरती, पर्याप्त सबूत इकट्ठा नहीं किए और अंत में मुख्य अभियुक्त कोर्ट से बरी हो गए.
सरकारी और ग़ैर-सरकारी संस्थाओं की रिपोर्टें इस तरफ़ इशारा करती हैं कि पुलिस सिस्टम में कमज़ोर तबकों को लेकर एक पूर्वाग्रह है और जाति उसका एक अहम हिस्सा है.
1997 में बिहार के लक्ष्मणपुर बाथे में 58 दलितों की हत्या का मामला हो, 2011 में हरियाणा का मिर्चपुर कांड हो या 2016 में गुजरात के उना में दलितों के साथ हिंसा का मामला, इन सभी मामलों में पुलिस पर जातिवादी पूर्वाग्रह के साथ काम करने का आरोप लगा.
बीबीसी की भी एक रिपोर्ट में ये सामने आया कि 14 साल की दलित लड़की के बलात्कार के मामले में पुलिस ने किस तरह जांच को प्रभावित किया. ऐसे कई मामलों में पुलिस शक़ के दायरे में रही है.

पुलिस सिस्टम में जातीय पूर्वाग्रह?
साल 2004 में आई मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट में ये स्पष्ट रूप से कहा गया कि पुलिस के अंदर एक जातीय पूर्वाग्रह है. अनुसूचित जाति के लोगों के साथ पुलिस का व्यवहार दिखाता है कि कहीं गहरे में जातीय पक्षपात छुपा है.
नेशनल दलित मूवमेंट फ़ॉर जस्टिस संस्था के राहुल सिंह कहते हैं कि अनुसूचित जाति के लोगों के लिए पहले कदम पर ही न्याय का रास्ता बंद कर दिया जाता है यानी उनकी शिकायत ही दर्ज नहीं होती.
अनुसूचित जाति-जनजाति आयोग ने अपनी रिपोर्ट में इस ओर ध्यान खींचा है कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की 2015 की रिपोर्ट में अनुसूचित जाति के लोगों के खिलाफ अपराध के 6009 मामलों में एससी-एसटी (प्रिवेंशन ऑफ़ एट्रोसिटी) एक्ट ही नहीं लगाया गया. न लगाने की वजह नहीं बताई गई है. आयोग ने कहा कि राज्य सरकारों को और गृह मंत्रालय को इसे जांचने की ज़रूरत है.
आयोग ने इस रिपोर्ट में पाया कि पुलिस शिकायत मिलने पर उसे एफआईआर में तब्दील करने से पहले शुरुआती जांच करने की बात कहती है इसलिए अनुसूचित जाति के पीड़ितों को कई मामलों में एफआईआर दर्ज करवाने के लिए भी कोर्ट से आदेश लाना पड़ता है जबकि सुप्रीम कोर्ट कई बार कह चुका है कि पहले एफआईआर दर्ज होनी चाहिए.
फिर बात आती है ग़लत सेक्शन में मामला दर्ज करने की. कई बार दलितों के अत्याचार के केस भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के तहत दर्ज कर दिए जाते हैं, जबकि उन्हें प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट, 1955 और एससी-एसटी एक्ट 1989 के तहत दर्ज किया जाना चाहिए.

इमेज स्रोत, HINDUSTAN TIMES VIA GETTY IMAGES
जांच के दौरान प्रक्रिया का पालन नहीं
एससी/ एसटी एक्ट ये भी कहता है कि मामले की जांच 60 दिनों में पूरी हो जानी चाहिए और इसी वक़्त में चार्जशीट भी दाखिल हो जानी चाहिए. लेकिन अक्सर ऐसा हकीकत में नहीं दिखाई देता.
एक्ट के सेक्शन 7 में ये अनिवार्य किया गया है कि इन मामलों में डीएसपी से नीचे की रैंक का अधिकारी जांच नहीं करेगा.
लेकिन नेशनल कैंपेन ऑन दलित ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट से पता चलता है कि ऐसा भी ज़मीन पर देखने को नहीं मिलता. उदाहरण के लिए तमिलनाडु के एक ज़िले विलुपुरम में 14 केस देखे गए जिनमें से ज़्यादातर में जांच अधिकारी डीएसपी नहीं थे.
क्या झूठे केस बनाए जा रहे हैं?
मार्च 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट में मामला दर्ज होते ही तुरंत गिरफ्तारी के प्रावधान को हटा दिया था. बल्कि अंतरिम ज़मानत का प्रावधान किया और केस दर्ज करने से पहले शुरुआती जांच करने का आदेश दिया.
कोर्ट का मानना था कि इस क़ानून का बेकसूर नागरिकों और सरकारी नौकरों को ब्लैकमेल करने के लिए दुरुपयोग किया जा रहा है.
हालांकि, इस आदेश पर काफ़ी हंगामा हुआ और सरकार ने इसे लागू नहीं किया.
दलित चिंतक एक बात ये भी कहते हैं कि जहां पुलिस अपराधियों को बचाना चाहती है, वहां जानबूझकर मुकदमों में देरी की जाती है. पुलिस के असहयोग और आर्थिक दिक्कतों की वजह से दलित पीड़ित एक-दो साल तो मुकदमा लड़ लेता है लेकिन उसके बाद केस छोड़ देता है.
खुद सरकार के सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे से ये बात सामने आती है कि इस एक्ट के अंतर्गत मामलों में पुलिस का एफआईआर दर्ज करने में देरी करना, गवाहों और शिकायतकर्ता का टूट जाना, अभियोजन पक्ष का मामले कोर्ट में ठीक से न रखने की वजह से भी अभियुक्त बरी हो जाते हैं.

इमेज स्रोत, Getty Images
भोपाल में वकालत कर रहीं निकिता सोनावणे कहती हैं, ''लोग कहते हैं कि क़ानून का दुरुपयोग हो रहा है लेकिन कानून और प्रक्रिया को तो लागू ही नहीं किया गया.''
निकिता कहती हैं कि अगर झूठे केस हैं तो वो झूठे केस पुलिस ने ही बनाए हैं. इसके पीछे भी निकिता एक जातीय पूर्वाग्रह देखती हैं.
वो कहती हैं, "ज़्यादातर जो चोरी के केस दर्ज होते हैं, उनमें आपको मुसलमान और डिनोटीफाइड ट्राइब्स पर मामले ज़्यादा दिखेंगे. पुलिस एक पूर्वाग्रह रखती है कि फलां अपराध ये वाला समुदाय करता है. उन्होंने वर्गीकरण कर रखा है कि कौन से अपराधी समुदाय हैं और कौन से समुदाय, कौन सा अपराध करते हैं."
निकिता जो बात कह रही हैं वो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट (2004) में भी सामने आई थी कि पुलिस के अंदर एक पूर्वाग्रह है कि दलित और आदिवासी जन्मजात आपराधिक प्रवृत्ति के होते हैं.
इसका एक हालिया उदाहरण है जब 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने डीनोटिफाइड ट्राइब के छह लोगों को बरी किया जिन्हें 10 साल पहले कोर्ट ने नासिक में डकैती, रेप और हत्या के मामले में फांसी की सज़ा दी थी. कोर्ट ने उन्हें बरी करते हुए कहा कि पुलिस ने उन पर झूठा मुक़दमा किया और असली गुनहगारों को जाने दिया. महाराष्ट्र सरकार को 5-5 लाख का मुआवज़ा देने का भी आदेश दिया.
लेकिन ये अकेला ऐसा उदाहरण नहीं है. तमिलनाडु में नरीकुरवा समुदाय एक डीनोटिफाइड ट्राइब है. 2014 में कन्याकुमारी में पुलिस पर आरोप लगा कि उसने इस समुदाय के 14 लोगों को गिरफ्तार कर यातनाएं दीं, 63 दिनों तक हिरासत में रखा जिनमें पांच बच्चे भी शामिल थे.
साल 2018 में महाराष्ट्र की पुलिस अफसर भाग्यश्री नवटके का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें उन्हें कहते सुना जा सकता है कि उन्होंने 21 दलितों के ख़िलाफ़ झूठे केस लगाए हैं जो एससी-एसटी एक्ट में रिपोर्ट लिखवाना चाहते थे. उन्होंने ये भी कहा कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ वह हत्या की कोशिश की धारा लगाती हैं ताकि उन्हें आसानी से ज़मानत ना मिल सके. उनके ख़िलाफ़ जांच भी बैठाई गई.
कॉमन कॉज़ और सीएसडीएस की 2019 की एक सर्वे रिपोर्ट में भी पुलिस का पूर्वाग्रह सामने आता है जिसके मुताबिक़ पांच में से एक पुलिसवाला ये मानता है कि एससी/एसटी एक्ट में दर्ज किए जाने वाले केस झूठे होते हैं और ज़्यादातर सवर्ण वर्ग के पुलिसवाले ऐसा मानते हैं.
अगर नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े देखें तो पता चलता है कि इस क़ानून के तहत झूठे मामलों का अनुपात बहुत कम है.
साथ ही, इस क़ानून के तहत दर्ज होने वाले मामलों में केस का निपटारा बहुत कम होता है. ज़्यादातर केस में अभियुक्त बरी हो जाते हैं.
नेशनल दलित मूवमेंट फ़ॉर जस्टिस संस्था के राहुल सिंह बताते हैं कि 2009 से लेकर 2018 तक स्पेशल कोर्ट में पहुंचे 25.2% मामलों का ही निपटारा हो पाया है. वहीं 62.5 फीसदी मामलों में अभियुक्त बरी हो गए.
यूएन कमेटी ऑन एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिसक्रिमिनेशन ने भी नोट किया है कि पुलिस दलित अत्याचार के मामलों में शिकायत दर्ज करने में अक्सर फेल होती है, जांच करने में फेल होती है. इसी वजह से अभियुक्तों के बरी होने की दर ज़्यादा है और सज़ा की दर कम है.

इमेज स्रोत, Getty Images
'पुलिस सिस्टम में जाति की भूमिका नहीं'
कई पूर्व वरिष्ठ पुलिस अधिकारी सिस्टम में जातीय पक्षपात से इनकार करते हैं.
उत्तर प्रदेश के पूर्व पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) बृजलाल ने बहुत स्पष्ट रूप से बीबीसी को बताया, "पुलिस में कोई जातिगत पक्षपात नहीं है. एक बार हम वर्दी पहन लेते हैं तो फिर कोई जाति वगैरह नहीं देखी जाती."
जब उनसे दोबारा पूछा कि क्या ये उनका आधिकारिक स्टैंड है, इस पर उन्होंने कहा कि 'सही स्टैंड ही यही है.'
बृजलाल उत्तर प्रदेश में मायावती सरकार में डीजीपी थे. सेवानिवृत्त होने के बाद वो 2015 में बीजेपी में शामिल हो गए. 2018 में वो उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग के अध्यक्ष भी बनाए गए.
वहीं, पुलिस सुधार के लिए लंबे समय से काम कर रहे पूर्व डीजीपी प्रकाश सिंह भी पुलिस में जातिगत पक्षपात की बात से इनकार करते हैं.
उन्होंने कहा, "शासन में जो पक्षपात होता है, वही पुलिस में नज़र आता है. उदाहरण के लिए, जब मायावती सरकार में आती हैं तो दलितों पर अत्याचार की बात तो दूर रही, बल्कि दलितों के ही अत्याचार करने की बात आने लगती है. जब यादवों की सरकार आती है तो यादव हावी हो जाते हैं."
"पुलिस में तो सभी जातियों के लोग हैं. आरक्षण की वजह से अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों की भर्ती काफ़ी हो गई है, बहुत लोग अफसर भी हैं. कुछ समझ नहीं आता है तो जातिगत पक्षपात की बात की जाती है."
हालांकि 2016 में हरियाणा के जाट आंदोलन के दौरान हुई हिंसा के बाद सरकार ने प्रकाश सिंह कमिटी को रिपोर्ट देने के लिए नियुक्त किया था. इस रिपोर्ट में उन्होंने ही लिखा था-
"पुलिस अफसरों ने या तो सरकार का सहयोग ना मिलने के डर से सख्त कार्रवाई नहीं की या अपने 'जातीय पक्षपात' की वजह से सख्ती नहीं दिखाई जिसकी वजह से ज़मीन पर दंगाइयों के खिलाफ़ कार्रवाई नहीं हुई, उपद्रवियों के साथ मिलीभगत दिखी, वे ड्यूटी से गायब दिखे और बदमाशों का हौसला बढ़ाया."

इमेज स्रोत, HINDUSTAN TIMES VIA GETTY IMAGES
महिला और वो भी दलित
उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक दलित लड़की के गैंगरेप का मामला कई दिन से सुर्खियों में है. उसी को लेकर बाराबंकी के एक भाजपा नेता रंजीत श्रीवास्तव का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर हो रहा है. जिसमें वो कह रहे हैं-
"लड़की ने लड़के को बुलाया होगा बाजरे के खेत में क्योंकि प्रेम प्रसंग था. सब बातें सोशल मीडिया पर भी हैं, चैनलों पर भी आ चुकी हैं. पकड़ ली गई होगी. अक्सर यही होता है खेतों में. ये जितनी लड़कियां इस तरह की मरती हैं, ये कुछ ही जगहों पर पाई जाती हैं."
पूर्व आईपीएस अधिकारी एसआर दारापुरी कहते हैं, "भारतीय समाज में महिला होना और दलित महिला होना, ये दोगुनी प्रतिकूल स्थिति है. दलित महिलाएं अपनी आर्थिक स्थिति की वजह से बाहर काम भी करती हैं. दूसरे के खेतों में, दूसरों के घरों में और वहां उनके ऊपर यौन हिंसा बहुत होती है. समाज के अंदर एक आम धारणा है कि दलित महिलाएं 'ऐसी ही' होती हैं और ऐसे में उनके साथ कुछ किया जाए तो वो गलत बात नहीं है. इसी मानसिकता के लोग पुलिस में भी हैं."
क्या पुलिस पर कार्रवाई हो सकती है?
प्रिवेंशन ऑफ़ एट्रोसिटी एक्ट का सेक्शन 4 कहता है कि कोई भी सरकारी अधिकारी जो एससी-एसटी नहीं है और वो जानबूझकर इस क़ानून के अंतर्गत ड्यूटी नहीं निभाता, तो उसके लिए सज़ा का प्रावधान है.
इसी साल 28 अप्रैल को दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने एक फैसले में ट्रायल कोर्ट को आदेश दिया कि वह इस सेक्शन के अंतर्गत पुलिस अधिकारियों के ख़िलाफ़ मुकदमा चलाए जिन्होंने एक दलित व्यक्ति की शिकायत दर्ज करने से मना कर दिया था.
तमाम रिपोर्ट्स के बावजूद पूर्व डीजीपी प्रकाश सिंह कहते हैं कि पुलिस अनुसूचित जाति के लोगों के केस दर्ज करने में कोताही नहीं बरतती क्योंकि शिकायत हो जाए तो बहुत सख्त कार्रवाई होती है.
वो ये भी कहते हैं, ''अब तो पुलिस वाले अनुसूचित जाति के लोगों से डील करने में घबराते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वे फर्ज़ी रिपोर्ट लिखवा देंगे तो गिरफ़्तारी भी अनिवार्य हो जाती है.''
वो कहते हैं, "पासा कुछ पलट-सा गया है."
हालांकि, पूर्व आईपीएस एसआर दारापुरी इस बात से सहमत नहीं हैं और वो पुलिसकर्मियों को विभाग के अंदर मिली 'इम्यूनिटी' के बारे में बताते हैं.
दारापुरी कहते हैं, "पुलिस वालों के एपीआर (सालाना परफॉर्मेंस रिव्यू) में कभी एडवर्स नहीं लिखा जाता है. अगर अनुसूचित जाति के लोग अपनी समस्या को लेकर मानवाधिकार आयोग या एससी-एसटी आयोग भी जाते हैं तो ये संस्थाएं भी कमज़ोर ही हैं. वे ज़्यादा से ज़्यादा राज्यों को शिकायत भेज देती हैं. राज्य एसपी को भेज देगा. बहुत कम केस में किसी को कोई सज़ा मिलती है. समस्या निवारण सिस्टम तो दलित और गैर-दलित दोनों में बहुत खराब है."

इमेज स्रोत, SUNIL GHOSH/HINDUSTAN TIMES VIA GETTY IMAGES
पुलिस ट्रेनिंग एक समस्या?
पुलिस ट्रेनिंग में जातीय और लैंगिक संवेदनशीलता के बारे में बताया जाता है लेकिन फिलहाल जो ट्रेनिंग है, उसे एसआर दारापुरी औपचारिकता भर मानते हैं.
उन्होंने बताया, "पुलिस में जातिवाद है. ये पूर्वाग्रह आसानी से नहीं जाते हैं. इसके लिए मज़बूत और नियमित ट्रेनिंग की ज़रूरत है. ब्रिटिश राज में एक थ्योरी थी कि 'कैच देम यंग' यानी 21 साल तक की उम्र के लोगों को ही पुलिस में भर्ती किया जाता था लेकिन अब 29 से 34 साल तक की उम्र में आईपीएस में एंट्री हो रही है. इस उम्र तक इंसान की सोच बहुत फिक्स हो जाती है और कुछ औपचारिक ट्रेनिंग उसे नहीं बदल सकती.
वोट-बैंक और नोट-बैंक
नेशनल कैंपेन ऑन दलित ह्यूमन राइट्स संस्था की राष्ट्रीय संयोजक प्रोफेसर विमल थोराट बताती हैं कि अनुसूचित जाति के ख़िलाफ़ अपराधों के मामले में पुलिस का जातिगत भेदभाव कैसे सामने आता है.
उन्होंने बताया, "सोनीपत में एक 11 साल की बच्ची के गैंगरेप में पुलिस की कार्रवाई के लिए भी हमें धरना देना पड़ा. बहुत सारे मामलों में देखा गया है कि जहां सवर्ण जाति के लोगों ने दलित बस्ती में आग लगाई हो तो पुलिस कहती है कि इन्होंने मुआवज़े के लिए खुद ही आग लगा ली. हमने खुद जाकर देखा है कि जिन मामलों में महिलाओं के हाथ-पैर तोड़े गए हैं उनमें पुलिस कहने लगती है कि इन लोगों ने खुद ही तोड़ लिए."
वे इन मामलों में पुलिस के काम में राजनीतिक हस्तक्षेप की भी बात करती हैं.
विमल थोराट कहती हैं, "राजनीतिक पार्टियों के लिए सवर्ण जाति के लोग वोट बैंक के साथ-साथ नोट-बैंक भी होते हैं. वैसी फंडिंग अनुसूचित जाति के लोग नहीं कर सकते. वो ग़रीब हैं तो सवर्ण जाति से आने वाले अपराधियों को कई बार राजनीतिक संरक्षण भी मिलता है और राजनीतिक हस्तक्षेप पुलिस को सही जांच करने से रोकता है."

इमेज स्रोत, Getty Images
पुलिस सिस्टम फेल होने से बढ़ता जातीय अहंकार
दिल्ली विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान के प्रोफ़ेसर सुकुमार नारायण कहते हैं, "जहां पुलिस सिस्टम फ़ेल होता है, वहां जातीय अहंकार और बढ़ता है क्योंकि अत्याचार करने वाला, बलात्कार करने वाला अपराध करके पीड़ित के सामने ही गांव में घूमता रहता है और कोई कुछ नहीं कर पाता."
प्रोफ़ेसर नारायण के अनुसार, "जाति, वर्ग और जेंडर का एक आपसी संबंध है जहां एक दलित पैसे वाला होगा, जिसके राजनीतिक कनेक्शन होंगे, उसे पुलिसकर्मी थोड़ी इज्जत देगा, भले ही न्याय पाने में मदद न करे."
वो कहते हैं कि कई बार पुलिस में दलित अफसर भी सिस्टम का हिस्सा बन जाता है, अभी जो लोग थोड़ा सवाल कर पा रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि संविधान है.
प्रोफ़ेसर नारायण कहते हैं, "लोग पुलिस को एक डर के तौर पर देखते हैं. खासकर दलित पुलिस को इस तरह से देखते हैं कि उनके पास जाने पर हम किसी मुसीबत में फंस जाएंगे. उनके दिल में ये डर रहता है कि पुलिस ऊंची जाति वालों के साथ ही खड़ी होंगे. हमारे साथ नहीं."
(बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए आप यहां क्लिक कर सकते हैं. आप हमें फ़ेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूबपर फ़ॉलो भी कर सकते हैं.)