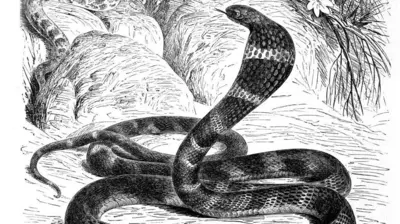बिहार चुनावः लाखों लोगों तक मनरेगा को पहुँचाने वाले एक मज़दूर भी हैं मैदान में

- Author, कीर्ति दुबे
- पदनाम, बीबीसी संवाददाता, बिहार से
मेड़ से थोड़ी ही चौड़ी सड़क है, सड़क के दोनों ओर धान की बालियां लहरा रही हैं. ये सीधी सड़क मुज़फ़्फ़रपुर के रतनौली गांव को जाती है. सड़क के किनारे छोटी सी किराना दुकान पर बैठे शख़्स से संजय सहनी के घर का पता पूछा तो जवाब मिला नरेगा वाले भईया के यहां जाएंगी ना... इसके बाद हमने कुछ क़दम नापे ही थे कि सामने एक तिरपाल में 40 से 50 लोग ज़मीन पर बैठे नज़र आए.
इनमें महिलाएं ज़्यादा और पुरुष कम हैं. लोगों से घिरे संजय सहनी लोगों को बता रहे हैं कि, "जो नेता कभी यहां आए ही नहीं दिल्ली में बैठे हैं उनके नाम पर हमेशा वोट माँग लिया जाता है. जिस नेता को सामने से देखे तक नहीं उनके लिए वोट करने को कहा जाता है."
नीली सफ़ेद धारियों वाली शर्ट, गहरे भूरे रंग की पतलून और काले रंग की स्लीपर पहने संजय सहनी असाधारण रूप से सफ़ेद कुर्ते और गेंदे के फूलों की माला से लदे नेताओं से बिलकुल अलग दिखते हैं. ना ही उनकी बातों में आम नेताओं सी लफ़्फ़ाज़ी है और ना ही नेताओं से तेवर.
उन्हें घेर कर बैठीं तमाम बूढ़ी-अधेड़ उम्र की महिलाओं के लिए वह किसी उम्मीदवार से ज़्यादा उनके संजय भईया हैं.
संजय सहनी मुज़फ़्फ़रपुर के कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं. संजय को अलमारी चुनाव चिन्ह मिला है.
वो बिहार चुनाव में सभी उम्मीदवारों से अलग हैं, इसलिए क्योंकि वो वादा नहीं कर रहे हैं कि जीतने पर वो क्या करेंगे बल्कि वो जो कर चुके हैं उसके आधार पर जनता के बीच उतरे हैं.
कुढ़नी विधानसभा में कुल 2,50,268 मतदाता हैं. 2015 के चुनाव में बीजेपी नेता केदार प्रसाद गुप्ता जीत कर विधायक बने और जेडीयू के मनोज कुशवाहा हारे. इस बार एनडीए से दोबारा केदार गुप्ता को टिकट मिला है और आरजेडी ने अनिल साहनी को अपना उम्मीदवार बनाया है.
जातीय समीकरण के हिसाब से इस सीट पर सहनी यानी मल्लाह लोगों की तादाद ज़्यादा है. इसके अलावा कुशवाहा लोगों की भी संख्या अच्छी है.

संजय से नरेगा वाले संजय भईया तक का सफ़र
संजय मनरेगा एक्टिविस्ट हैं और ख़ुद मनरेगा मज़दूर भी हैं, लेकिन मज़दूर संजय सहनी से संजय भईया बनने का सफ़र आठ साल पुराना है.
सातवीं तक पढ़ाई करने वाले संजय दिल्ली के जनकपुरी इलाक़े में मज़दूरी करते थे. इस दौरान उनका वास्ता इंटरनेट से हुआ. ये वो वक़्त था जब फ़ोन में फ़्री डाटा नहीं मिलता था बल्कि साइबर कैफ़े का चलन हुआ करता था.
एक दिन संजय अपने गांव के बारे में इंटरनेट पर कुछ पढ़ रहे थे. इस दौरान उन्हें एक दस्तावेज़ मिला जिसमें उनके गांव के लोगों के नाम थे. ये रतनौली गांव के मनरेगा मज़दूरों की सूची थी.
संजय जब घर वापस आए तो उन्होंने गांव वालों से पूछा कि क्या उन्हें मनरेगा के तहत काम मिल रहा है तभी उन्हें पता चला कि उनके गांव में किसी को मनरेगा की जानकारी भी नहीं है. यानी उनके नाम पर मज़दूरी तो हो रही है लेकिन उनतक नहीं पहुँच रही.
और यहीं से संजय ने अपने इलाक़े में मनरेगा की धांधली के नेक्सस को उजागर किया. उन्हें पता चला कि जॉब कार्ड बना कर पैसे उठाए जा रहे हैं लेकिन वो पैसे मज़दूरों तक नहीं आ रहे बल्कि ब्लॉक अधिकारी और बिचौलिए आपस में बाँट ले रहे हैं.
2012 में वह दिल्ली में इलेक्ट्रिशियन का काम छोड़कर रतनौली वापस आ गए.
साल 2013 में संजय ने समाज परिवर्तन शक़्ति संगठन-मनरेगा वॉच बनाया, जिसका काम लोगों में मनरेगा को लेकर जागरूकता लाना था.
लेकिन नेक्सस उजागर हुआ तो कई लोगों की आंखों में संजय और उनकी टीम खटकने लगी. साल 2014 में संजय सहनी के ख़िलाफ़ एफ़आईआर दर्ज हुई. आज उनपर लोगों से जबरन काम कराने, हत्या जैसे केस हैं.
लेकिन संजय का संगठन मनरेगा के लिए लगातार काम करता रहा है. अपने गांव से शुरू हुआ सफ़र अब 300 से ज़्यादा गांवों में फैल चुका है. संजय दावा करते हैं कि उन्होनें सवा लाख लोगों को मनरेगा में काम दिलाया है.

'मज़दूर तो हर जाति में होता है ना'
बिहार जैसे राज्य में जहां राजनीति में जातीय समीकरण काम करते हैं, संजय कैसे चुनौती देंगे? इस सवाल पर वह बीबीसी से कहते हैं, "ये बात ठीक है कि बिहार में आज तक जाति के नाम पर वोट दिए जाते हैं लेकिन हमारा सिस्टम अलग है. मैं ख़ुद मज़दूर हूं और मज़दूर हर जाति में होते हैं और उनका संघर्ष भी एक ही होता है."
"बिहार का ये इतिहास बदलना है, नेता जाति की बात करेंगे, जाति पर समर्थन मांगेंगे और जीतते भी रहे हैं लेकिन हम मुद्दों पर बात कर रहे हैं और ये हमारी परेशानियां हैं न कि जाति."
संजय के पास दूसरे नेताओं जैसे बड़ी-बड़ी रैलियां करने के पैसे नहीं है, लेकिन उनका घर इस वक़्त एक 'कम्यून' में तब्दील हो चुका है. आस-पास के गांव से उनके समर्थन में आईं औरतें उनके घर पर ही रहती हैं, उनके घर पर ही ये औरतें अपना खाना बनाती हैं और दोपहर के वक़्त संजय सहनी के साथ इलाक़े में उनका प्रचार करने जाती हैं.
संजय बताते हैं, "मेरे पास पैसे नहीं है. 15 हज़ार रुपये हैं जो चुनाव आयोग को बताया है. इस चुनाव का पूरा ख़र्चा मेरे ग़रीब मज़दूर गांव वाले चंदा देकर उठा रहे हैं."
उनके घर पर जिन लोगों का खाना बनता है उसका राशन भी गांव वालों की मदद से जुटाया जाता है. संजय कहते हैं कि 'सबको पता है मेरे पास पैसे हैं ही नहीं तो ख़र्च कैसे करूंगा.'

'हमार मज़दूर विधायक हमन ख़ातिर ठड़ा (खड़ा) होंगे'
ग्रामीण भारत को क़रीब से समझने वाले जाने माने अर्थशास्त्री ज्यां द्रेज़ संजय सहनी की उम्मीदवारी को भारत की चुनावी राजनीति का एक सकारात्मक बदलाव मानते हैं.
वे कहते हैं, "मनरेगा का काम सिर्फ़ लोगों को काम देना नहीं था. ये एक काम था. इसके अलावा लोगों को संपूर्ण अधिकार मिले, ऐसे लोग लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हिस्सा लें, ये ज़रूरी है. संजय सहनी के चुनावी मैदान में आने की प्रक्रिया बेहद ख़ूबसूरत है, वे ख़ुद मज़दूर रहे हैं और जिन मज़दूरों ने उनके साथ संघर्ष किया वो अपने में से किसी को चुनना चाहते हैं, इससे बेहतर सोच क्या होगी."
दोपहर के दो बजे हैं, संजय अपनी चुनावी सभा के लिए महंत मनियारपुर गांव जाने को तैयार हैं, उनकी चुनावी यात्राओं के लिए तीन विक्रम टैम्पू आए हैं. एक टैम्पू ख़ुद संजय चलाते हुए अपनी महिला मज़दूर साथियों के साथ सभाओं के लिए निकलते हैं.
टैम्पू में बड़े लाउडस्पीकर में गाना बज रहा है. जिसके बोल हैं- संजय सहनी जी हऊने भईया… ये गाना किसी पीआर टीम ने नहीं बनाया बल्कि उनके एक समर्थक ने उन्हें भेंट दिया है. भारत में चुनाव लड़ना भी एक मंहगी प्रक्रिया है, लेकिन संजय की जन सभाएं इन मान्यताओं को ठेंगा दिखाती हैं.
टैम्पू आगे बढ़ जाती है और गाने की आवाज़ हवाओं में घुल जाती है.
इस बीच पीछे से एक आवाज़ आती है, "निकर गईल का....हम रही गईलीं."

ये आवाज़ मंदेसरी देवी की है. मंदेसरी भी उन महिलाओं में से एक हैं जिनके हाथों में मनरेगा ने कुदाल थमाई और उनका पेट भरा.
ये पिछड़े बिहार की वो मज़बूत महिलाएं हैं जो ख़ुद अपने गांवों से चल कर यहां तक आई हैं और संजय को अपना नेता मानती हैं.
मंदेसरी अब एक मोटरसाइकिल का इंतज़ार कर रही हैं ताकि संजय की सभाओं का हिस्सा बन सकें.
गाड़ी का इंतज़ार करते हुए वो हमसे बात करने लगती हैं. वह बताती हैं कि आठ साल पहले उन्हें पहली मज़दूरी संजय सहनी के कारण मिली. उससे पहले उन्हें मनरेगा के बारे में कुछ भी पता नहीं था.
वे कहती हैं, "संजय जी आठ साल पहले गांव आए तो बताए कि नरेगा एक चीज़ है जिसमें मनई-मज़दूर खट के पेट भर सकते हैं. हमको संजय जी ने अधिकार दिया दिल्ली से वापस आ कर हमें बताए. हम संजय जी के साथ बहुत संघर्ष किए और फिर हमको काम मिला. हमार मज़दूर विधायक हमन ख़ातिर ठड़ा (खड़ा) होंगे तो हमारी बात ऊपर तक पहुंचाएँगे ना."
मंदेसरी की पढ़ाई लिखाई नहीं हुई. उन्हें अपनी उम्र भी ठीक-ठीक नहीं पता. लेकिन वो उन चंद लोगों में से हैं जिन्हें इस साल मनरेगा के ज़रिए थोड़ा ही सही लेकिन काम मिला.
वे बताती हैं, "हमको आख़िरी बार आषाढ़ में काम मिला था."
लेकिन मंदेसरी जैसी कई सारी महिलाएं हैं जिनको किसी संजय सहनी ने मदद नहीं की.

इंतज़ार, मजबूरी और बड़े शहरों में वापसी
बिहार के ज़्यादातर हिस्सों में मज़दूर काम के लिए तरस रहे हैं. ग्रामीण इलाक़ों से बस एक शब्द ही बार-बार सुनाई पड़ता है और वो है 'काम-मज़दूरी'.
नालंदा ज़िले के कल्याण बिगहा गांव के रहने वाले नवलेस राम मद्रास में लोहा पिघलाने का काम करते थे, लेकिन इस साल अप्रैल में जब मालिक ने पैसे नहीं दिए तो उनके पास अपने गांव वापस आने के अलावा कोई और चारा नहीं था. कुछ चंद जुटाए रुपयों से बस की छत पर बैठकर बिहार वापस आ गए.
नवलेस एक ज़मींदार के खेत में बीते दो दिन से धान काट रहे हैं. उनके हाथ में हसिया है और पूरा बदन धान की भूसियों से सना हुआ है.
मुझे देखते ही उनका दुख फूट पड़ता है. वह कहते हैं, "हम तो काम ढूंढ रहे हैं. हम कैसे वापस आए हैं ये हम ही जानते हैं. डर लगता है, वापस गए और फिर लॉकडाउन हो जाए तो... इस बार तो ज़िंदा बच गए, अपने गांव आ गए लेकिन क्या पता फिर लॉकडाउन हो और वापस न आ पाएं."
"कोई नेता हमारा दर्द समझता है क्या, समझ नहीं आता है किसको वोट दें."
ये कहते हुए उनकी आंखों में ग़ुस्से के साथ-साथ लाचारी भी नज़र आती है. नवलेस जहां धान काट रहे हैं उन्हें उसके पैसे नहीं मिलेंगे. ये सौदा खेत में मज़दूरी करने और कुछ किलो धान पाने का है.
इस साल मार्च से लगे लॉकडाउन के कारण लाखों प्रवासी मज़दूर बिहार वापस आए.
सितंबर में सरकार ने लोकसभा में बताया कि देशभर में एक करोड़ प्रवासी मज़दूर लॉकडाउन के दौरान अपने राज्य वापस गए. इनमें से 15 लाख प्रवासी मज़दूर बिहार के थे.

हालांकि ये डेटा उन मज़दूरों का है जो ट्रेन से बिहार लौटे. जो मज़दूर मीलों पैदल चलकर या ट्रकों-ट्रेनों से अपने गांवों तक पहुंचे उनकी संख्या और भी ज़्यादा है. ऐसे मज़दूरों के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी अधिनियम ही रोज़ी-रोटी का सबसे बड़ा सहारा था लेकिन इन मज़दूरों की दुश्वारियों का कोई अंत नहीं दिखता.
मुज़फ़्फ़रपुर के किनारु गांव के एक खेत में राजू मांझी धान के गट्ठे बांध रहे हैं. आज दिन का मेहनताना पाने के लिए उन्हें ऐसे ही सात गट्ठे और बांधने होंगे.
राजू एक प्रवासी मज़दूर थे लेकिन अब वो बेहद कम पैसे में एक ज़मींदार की धान की फ़सल काट रहे हैं. छह बड़े कट्ठे काटकर बांधने पर उन्हें दिन का 200 रुपया मिलेगा. ये काम भी उन्हें एक सप्ताह पहले ही मिला है.
राजू मैंगलोर में काम करते थे लेकिन लॉकडाउन में जिस ठेकेदार के ज़रिए वो पराए देश गए थे उसने सात महीने का बक़ाया वेतन नहीं दिया.
राजू बताते हैं, "ठेकेदार 10 हज़ार महीना के काम पर ले गया लेकिन बड़े शहर पहुँचते ही उसने बातें बदल लीं. सात महीने काम किए और जब हिसाब किया तो छह हज़ार रुपये महीना का हिसाब किया."
"राजू अपने घर आए तो ठेकेदार ने कहा कि घर जाओ खाता में डाल देंगे लेकिन पैसा अब तक आया नहीं."
राजू होली में अपने गांव आए थे लेकिन फिर लॉकडाउन लगा और न ही उन्हें अपना मेहनताना मिला और न ही कोई दूसरा काम.
कई कोशिश के बावजूद उनका मनरेगा का कार्ड भी नहीं बन पाया है. धान की कटाई का सीज़न अक्तूबर बाद नहीं होगा और उसके बाद क्या होगा, उन्हें नहीं पता.
पेट की आग ऐसी है कि वह पराए देस में हुई अपनी दुर्दशा को भुलाकर दोबारा वहीं जाना चाहते हैं, लेकिन इस बार वो मैंगलोर नहीं सिलचर जाएंगे.
राजू कहते हैं, "डर तो बहुत लगता है, जो देखे हैं उसके बाद हिम्मत नहीं पड़ती है लेकिन का करें तीन गो बच्चा है, पत्नी है. यहां काम मिलता को भला क्यों जाते. हम त ग़रीब मनई हैं, जो काम मिलेगा कर लेंगे, फ़ैक्ट्री में, खेत में. वहां जाते हैं तो भी पैसा कहां मिलता है, अच्छा खाने को भी नहीं मिलता लेकिन नून-चावल (नमक-चावल) खिलाना है तो जाना पड़ेगा ही."
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार से अनुरोध किया कि साल के 100 श्रम दिवस की अधिकतम सीमा को 200 दिन किए जाएं. हालांकि इस माँग पर केंद्र सरकार ने कोई फ़ैसला नहीं लिया है. लेकिन क्या मौजूदा वक़्त में मज़दूरों को 100 दिन भी काम मिल पा रहा है? इसका जवाब है, नहीं.

मनरेगा की वेबसाइट पर मौजूद सरकारी आंकड़े बताते हैं कि इस वित्तीय वर्ष 2020-21 में बिहार में अब तक मज़दूरों को औसतन महज़ 33 दिन काम मिला है. 2019-20 में 41 दिन काम मिला, 2018-19 में 42 दिन काम मिला, 2017-18 में मात्र 36 दिन काम मिला.
यानी बीते कई सालों से मज़दूरों को औसतन 50 दिन भी काम नहीं मिल पाया है.
साल 2020-21 के अक्तूबर महीने तक कुल 37 लाख हाउस होल्डस को मनरेगा के तहत काम मिला जिनमें से महज़ पाँच हज़ार ऐसे हाउसहोल्ड्स हैं जिन्हें 100 दिन का रोज़गार मनरेगा के तहत मिला है.
बिहार में बीजेपी, जेडीयू और आरजेडी के घोषणापत्र में रोज़गार के वादे किए गए हैं लेकिन एक क़ानून जो पहले से ही ग़रीबों के लिए है, उन पर पार्टियां बात तक नहीं करतीं.
क्या कहती है बिहार सरकार
बिहार में मज़दूरों को मनरेगा के तहत काम ना मिलने और राज्य का बजट ख़त्म होने के सवाल पर बिहार के ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव अरविंद कुमार चौधरी कहते हैं, ''ऐसा नहीं है कि बिहार में लोगों को मज़दूरी नहीं मिल रही है, मनरेगा का काम मिल रहा है. पेमेंट को लेकर देरी हो जाती है. मुझे उम्मीद है कि इस हफ़्ते तक भुगतान हो जाएगा.''
वे कहते हैं, "सोमवार को हमारे डेटा के मुताबिक़ 6 लाख मज़दूरों ने काम किया है. देखिए ये एक प्रक्रिया है. केंद्र सरकार राज्य सरकार को कुछ तय पैसे मदर एलोकेशन के तौर पर देती है. जब यह पैसा ख़त्म होता है, तो हम रिपोर्ट भेजते हैं राज्य की, फिर उस मदर एलोकेशन को बढ़ाया जाता है. इस बार हमने 76% अपने बजट का इस्तेमाल कर लिया है.''
मज़दूरों के पलायन पर वे कहते हैं, "अगर कोई बेहतर वेतन की तलाश में जा रहा है, तो इसमें ग़लत कुछ भी नहीं, हम भी बच्चों को विदेश और बड़े शहर भेजते हैं ताकि उन्हें बेहतर शिक्षा मिले. लेकिन इसे डिस्ट्रेस माइग्रेशन नहीं माना जा सकता. इसके बावजूद हमारा टोल फ़्री नंबर है हमारी वेबसाइट पर. हम तक जानकारी पहुँचाई जाए, हम मदद करेंगे."
मनरेगा का ज़िक्र न मोदी करते हैं, न ही तेजस्वी
चुनाव से बिहार के ग़रीबों का सबसे बड़ा मुद्दा आख़िर ग़ायब क्यों है? अन-स्किल्ड बेरोज़गार मज़दूरों की बात चुनाव में क्यों नहीं हो रही?
इस सवाल पर ज्यां द्रेज कहते हैं, "मोदी सरकार का रुख़ मनरेगा को लेकर बड़ा कश्मकश भरा रहता है. उन्हें पता है कि मनरेगा की माँग बहुत ज़्यादा है ख़ासकर इस साल जब कई लोग अपनी नौकरी लॉकडाउन में गंवा चुके हैं, ऐसे में उन्हें अपने गांवों में ही मनरेगा से काम मिलेगा. मोदी सरकार एक तरफ़ मनरेगा की माँग को लेकर कुछ क़दम तो उठाती है लेकिन दूसरी तरफ़ वो ये मानती है कि मनरेगा का क्रेडिट मोदी को नहीं मिलेगा क्योंकि ये यूपीए का लाया हुआ क़ानून है, ऐसे में सरकार कोई प्रभावी क़दम नहीं उठाती."
बिहार के चुनाव में कुल 274 लाख लोगों को रोज़गार देने वाली मनरेगा का ज़िक्र न तो प्रधानमंत्री मोदी अपनी रैलियों में करते हैं और न ही तेजस्वी यादव.

मनरेगा की हक़ीकत और सरकारों के लिए क्रेडिट का खेल
इस साल फ़रवरी में 2020-21 के बजट में क्रेंद्र सरकार ने 60 हज़ार करोड़ का फ़ंड मनरेगा के लिए आवंटित किया. ये रक़म 2019-20 के बजट से 13 फ़ीसद कम थी. हालांकि मई में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रवासी मज़दूरों के संकट को देखते हुए 40 हज़ार करोड़ के अतिरिक्त बजट का एलान किया.
ज्यां द्रेज़ इस तरह के फ़ंड की सीमा तय करने की प्रक्रिया को उचित नहीं मानते.
वह कहते हैं, "ये रक़म बेहद कम है. ऐसे में इस साल भी वही होने वाला है जो हर साल होता है. मनरेगा का फ़ंड वित्तीय वर्ष ख़त्म होने से पहले ही ख़त्म हो जाता है. फिर होता ये है कि मज़दूर अपना काम करता है और उसे उसके पैसे नहीं मिलते. फिर जब नया वित्तीय बजट आता है तो मज़दूर का वेतन आता है, जबकि नियम कहता है कि 15 दिन के भीतर मनरेगा मज़दूरों को उनकी मज़दूरी मिल जानी चाहिए."
"इस बार तो ऐसा और भी ज़्यादा होने के आसार हैं क्योंकि लोगों के पास कोई काम नहीं है, लोग बिना भुगतान भी काम करेंगे और ये उनके साथ सबसे बड़ा अन्याय होगा."
"ये याद रखना होगा कि मनरेगा माँग पर आधारित स्कीम है. काम की माँग के आधार पर फ़ंड का आवंटन होना चाहिए न कि फ़ंड के आवंटन के आधार पर काम मिलना चाहिए. ऐसे में फ़ंड की सीमा तय करने का मतलब है, लोगों को बिना भुगतान काम करना होगा."
माइनस में बिहार मनरेगा का बजट
देशभर में मनरेगा मज़दूरों के लिए काम करने वाले नेटवर्क पीपुल्स एक्शन फ़ॉर एम्प्लॉयमेंट गारंटी यानी पेज की रिपोर्ट के मुताबिक़ एक लाख करोड़ की रक़म भारत की कुल जीडीपी (2019-20) 204.42 लाख करोड़ का महज़ 0.5 फ़ीसद है. जबकि वर्ल्ड बैंक की अर्थशास्त्री रिंकू मुरुगई और मार्टिन रेवेलियन जैसे लोगों का मानना है कि मनरेगा को प्रभावी बनाने के लिए कुल जीडीपी का 1.7% हिस्सा मिलना चाहिए, ये रक़म लगभग 3.5 लाख करोड़ होगी यानी मौजूदा फ़ंड का तीन गुना.
पेज नरेगा ट्रैकर की रिपोर्ट कहती है कि एक लाख करोड़ के बजट में से 43% यानी 43,717 करोड़ 2020-21 की पहली तिमाही में ही इस्तेमाल हो चुका है. बिहार ने तो अपनी पहली तिमाही तक 91% फ़ंड का इस्तेमाल कर लिया है. दूसरी तिमाही के ख़त्म होने से पहले ही बिहार में मनरेगा का बजट नेगेटिव में जा चुका था, वर्तमान समय में राज्य का बजट माइनस 159 करोड़ पहुँच चुका है. जबकि वित्तीय वर्ष ख़त्म होने में चार महीने बाक़ी हैं.
नतीजा ये है कि बिहार में इस वक़्त मनरेगा के तहत कोई मज़दूर काम नहीं कर रहा है.
मनरेगा मज़दूरी क्यों नहीं बढ़ाती सरकार?
मनरेगा में मिलने वाली मज़दूरी इस स्कीम को लगातार कमज़ोर कर रही है. मनरेगा में मिलने वाली मज़दूरी कई राज्यों में तय न्यूनतम मज़दूरी से भी कम है. बिहार की बात करें तो बिहार की न्यूनतम मज़दूरी अकुशल मज़दूर (अनस्किल्ड लेबर) के लिए रोज़ाना 287 रुपये हैं, लेकिन मनरेगा मज़दूर को केवल 193.87 रुपये मज़दूरी मिलती है.
ज्यां द्रेज मानते हैं, "आने वाले वक़्त में मनरेगा को बेहतर बनाने के लिए सरकार को न्यूनतम वेतन क़ानून के तहत केंद्र सरकार को ये वेतन बढ़ाना चाहिए. केंद्र को राज्यों को न्यूनतम वेतन बढ़ा कर देना चाहिए. दरअसल केंद्र सरकार को लगता है कि अगर वो राज्य का न्यूनतम वेतन बढ़ाएगी तो राज्य सरकार भी न्यूनतम वेतन बढ़ा देंगे. मुझे नहीं लगता कि सरकार का ये डर उचित है क्योंकि राज्य सरकार ख़ुद भी मज़दूरी देती हैं तो वे ऐसा क्यों करेगी."

कई बार मज़दूरों का पेमेंट रिजेक्ट हो जाता है और इसके कई कारण हो सकते हैं, आधार की ग़लत मैपिंग से लेकर अकाउंट नंबर में गड़बड़ी तक. एक रिपोर्ट बताती है कि देश भर में 23 में से एक वेतन भुगतान फ़ेल हो जाता है और इसका कारण आधार की ग़लत मैपिंग जैसी टेक्नॉलॉजी की परेशानियां होती हैं.
कई बार मज़दूर ये तक नहीं समझ पाते कि आख़िर गड़बड़ी कहां है और इस तरह उनकी पेमेंट बार-बार रिजेक्ट होती जाती है, वे बिना भुगतान काम करते जाते हैं.
पेज की रिपोर्ट बताती है कि 2020-21 में अब तक 36.02 करोड़ मज़दूरों की पेमेंट रिजेक्ट की जा चुकी है और इसमें मज़दूरों की कोई ग़लती नहीं है. ऐसा टेक्नीकल कारणों से हो रहा है.
साल 2016-17 से लेकर 2019-20 तक 98.78 करोड़ वेतन राशि का भुगतान नहीं हो सका.
पलायन करने को मजबूर मज़दूर
मुज़फ़्फ़रपुर के मुसहरी में रहने वाली पवन देवी मनरेगा के तहत मज़दूरी करती हैं. इस साल उनको आठ दिन ही काम मिला. पवन देवी के बेटे मुकेश सिलचर के एक ईंट भट्टे पर काम करते हैं, लेकिन लॉकडाउन में भट्टा बंद हो गया और मालिक ने पैसे भी नहीं दिए. कई दिनों की कोशिशों के बाद वे अपने इलाक़े के 55 अन्य लोगों के साथ ट्रक में बैठकर मुज़फ़्फ़रपुर आए. मुकेश को पाँच हज़ार का किराया भरना पड़ा. बेटे को वापस बुलाने के लिए पवन देवी ने अपनी भैंस बेच दी. वो भैंस जो इस बुरे वक़्त में उनकी आमदनी का बड़ा ज़रिया थी.
मुकेश अब वापस ईंट के भट्टे पर काम करने के लिए सिलचर चले गए हैं. पवन देवी कहती हैं, "ईंहा हमको आठ दिन काम मिला ऊ का करता. ईंहा भट्टा पर काम करता तो 1000 ईंटा का 500 रुपया सेठ देता, अब जहां गया है ऊंहा 1000 ईंटा पारेगा (बनाएगा) तो 1000 रुपया देगा."
बिहार में ऐसे कई परिवार मिले जिनके घर वापस आए लोग वापस बड़े शहरों का रुख़ कर रहे हैं. इसकी बड़ी वजह है लोगों का काम के लिए लंबा इंतज़ार और नाउम्मीदी.

आत्मनिर्भर बिहार, लेकिन कैसे?
बिहार के चुनाव में नेता कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने पर, राम मंदिर बनवाने पर अपनी उपलब्धि तो बता रहे हैं लेकिन ये कोई नेता नहीं बता रहा कि राज्य प्रवासी मज़दूरों को राहत कैसे पहुँचाएगा. कोई उस मज़दूर की बात नहीं करता जिसकी बिलखती तस्वीर ने सरकार और समाज की करतूतों की क़लई खोल दी थी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भागलपुर की रैली में आत्मनिर्भर बिहार बनाने की बात कही.
ज्यां द्रेज कहते हैं, "मोदी सरकार ने आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया है. ये ठीक जुमले जैसा है, कॉरपोरेट घरानों के लिए सरकार ने काम किया है, हो सकता है वो आत्मनिर्भर बन जाएं लेकिन ग़रीबों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए क्या किया गया है. बीते छह सालों में सामाजिक सुरक्षा को लेकर शायद ही कोई क़दम उठाया गया है. आख़िरी बार साल 2013 में ग़रीबों को सामाजिक सुरक्षा देने के लिए अहम बिल 'नेशनल फ़ूड सिक्योरिटी एक्ट' लाया गया था. मनरेगा को लेकर सरकार की अनिच्छा साफ़ नज़र आती है."
चुनाव से ठीक पहले 125 दिन वाली ग़रीब कल्याण योजना
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 जून को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए बिहार के खगड़िया में ग़रीब कल्याण रोज़गार अभियान लॉन्च किया. 125 दिन की इस योजना का बजट 50 हज़ार करोड़ रखा गया है. इसके जरिए 116 ज़िलों में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा. इस योजना को छह राज्यों में लागू किया गया है. बिहार के 32 ज़िलों का नाम इस योजना की लिस्ट में रखा गया है.
बिहार के सर्वाधिक ज़िले इस योजना का हिस्सा हैं.
ग्रमीण विकास मंत्रालय की वेबसाइट पर मौजूद डाटा के मुताबिक़, अब तक ग़रीब कल्याण योजना में 33,378 करोड़ ख़र्च किए चा जुके हैं. हालांकि हर राज्य में कितना ख़र्च हुआ है, इसका डाटा उपलब्ध नहीं है.
इस पर सवाल ये उठता है कि जिन 32 ज़िलों में ग़रीब कल्याण योजना लागू हुई है, वहां क्या मज़दूरों को मनरेगा का काम मिल पा रहा है?

इसका जवाब देती हैं पेज की 31 अगस्त, 2020 की रिपोर्ट. बिहार के जिन ज़िलों में ग़रीब कल्याण योजना लागू है वहां एक घर से एक आदमी को 31 दिन काम मिला, वहीं जिन राज्यों में ये योजना लागू नहीं है वहां 32 दिनों का काम एक हाउस होल्ड को दिया गया. यानी जिन ज़िलों में ग़रीब कल्याण अभियान चल रहा है उसमें और जिन ज़िलों में ये नहीं है, दोनों में कोई अंतर नज़र नहीं आता.
लॉकडाउन के कारण दिल्ली से अपने गांव चिटोरिया पंचायत, कटिहार वापस आए अरुण यादव को अब अपने गांव और अपने लोगों के बीच रह कर काम करने की कोई उम्मीद नज़र नहीं आती.
वह बताते हैं, "जब हम दिल्ली से वापस आए तो दो सप्ताह क्वारंटीन सेंटर में रखा गया. वहां सरकारी अधिकारी आए, मेरी जानकारी ली और वादा किया कि प्रवासी मज़दूरों को काम देंगे. इसके बाद गांव के मुखिया ने वृक्षारोपण में काम दिलाया. हम लोगों को बताया गया कि 194 रुपये मनरेगा वेतन मिलेगा लेकिन 30 दिन काम करने के बाद हमको 50 रुपये रोज़ाना के हिसाब से पैसे दिए गए और कहा गया कि सरकार 50 रुपये ही दे रही है. हम मनरेगा वेतन माँगे लेकिन नहीं मिला. हम ग़रीब कल्याण रोज़गार अभियान में भी गए. बताया गया कि सरकार से फ़ोन आएगा लेकिन 50 दिन बीत गए कोई फ़ोन नहीं आया. नौकरी तो करना ही है तो अब दिल्ली वापस लौट जाएंगे."
मनरेगा ठेकेदार और लोकल नेताओं का नेक्सस
आम मज़दूरों से बात करके हमने ये पाया कि बहुतेरे मज़दूर जो मनरेगा के तहत काम करते हैं उन्हें पहले तो महीनों इंतज़ार करना पड़ता है और जब इंतज़ार ख़त्म होता है तो मिलने वाले पैसे में से ठेकेदार कमिशन काट कर देते हैं.
किनारु गांव में धान के एक खेत में हसुआ चलाते हुए बुधिया देवी मनरेगा क्या होता है ये नहीं जानतीं पर इस स्कीम को वे 'कार्ड वाला काम' के नाम से जानती हैं.
वह कहती हैं, "हां कार्ड है बाक़ी काम ना मिले बिटिया, पर-परियार साल बैसाख में मिलल रहे बाक़ी पईसा ना मिलल. (हमारे पास कार्ड है लेकिन पिछले के भी पिछले साल अप्रैल/मई में काम मिला था लेकिन पैसे नहीं मिले थे)."
"वोट लेने सब जने आवत हैं... आ जीत जात हैं... ते तो अपने घरे चल जात हैं इ लोग. ग़रीब के देखे केहू आवत है का, जीता द आ ग़रीब रहे आपन झोपड़ी में. जौन कमाइल जा ला उम्मे से ठेकेदारों ना पइसा लेला आ जौन तनी मनी मिलेला उहे मिलेला." (वोट लेने नेता आते हैं लेकिन जब जीत जाते हैं तो अपने घरों में रहते हैं, ग़रीब को देखने कौन आता है. ग़रीब अपने झोपड़ी में रहता है. जो कमाते हैं उसमें से ठेकेदार पैसे ले लेता है और इसके बाद जो बचता है वही मज़दूरी हमारी होती है.)
पहले तो मज़दूरों को ज़रूरत भर काम नहीं मिल पा रहा है और जिन्हें मिल रहा है वे ठेकेदारों-बिचौलियों के चंगुल में फँस कर रह जा रहे हैं.

ज्यां द्रेज मानते हैं कि मज़दूरों को 15 दिन में वेतन मिलना बेहद ज़रूरी है. साथ ही वह कहते हैं, "बिहार और झारखंड जैसे राज्य जहां मनरेगा की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वहां मनरेगा को ठीक से लागू नहीं किया जा रहा है. सबसे ज़रूरी है मनरेगा से बड़े ठेकेदारों को हटाया जाए. ओडिशा और छत्तीसगढ़ में मनरेगा ठेकेदारों को पूरी तरह ख़त्म कर दिया गया है. वहां इसे लागू कराने का काम ग्राम पंचायतों का है और यक़ीनन यही मनरेगा को इसके असली रूप में लोगों तक पहुँचाने का सही तरीक़ा है."
"लेकिन बिहार और झारखंड में कई ठेकेदार हैं जिनकी मनरेगा में कोई भूमिका नहीं है फिर भी वे स्थानीय नेताओं के साथ मिलकर ग़रीब मज़दूरों को लूट रहे हैं और ये लूट तब तक चलती रहेगी जब तक ये बिचौलिए मज़दूरों और उसे काम देने वाले के बीच मौजूद रहेंगे."
कोरोना वायरस के कारण हुए लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मज़दूरों का पैदल भूखे-प्यासे अपने गांवों को निकल जाना बीते कई सालों का सबसे दर्दनाक पलायन रहा. एक ऐसा मानवीय संकट जिसे बिहार चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए उसकी चर्चा तक नहीं की जा रही.
नालंदा में हमसे 70 साल की देवादेवी मांझी ने कहा था, "ग़रीबन का कौउन मुद्दा होला मैडम, बड़का जनि के परसानी रही त नेता बोलिहें ग़रीबन के कउन पूछा (ग़रीब आदमी का कौन सा मुद्दा होता है, मुद्दे शक्तिशाली लोगों की परेशानियां बनते हैं. ग़रीब को कौन पूछता है.)
देवादेवी की ये एक पंक्ति ही बिहार सहित उत्तर भारत में प्रवासी और मनरेगा मज़दूरों की अंतहीन दर्द और इंतज़ार में डूबी कहानी की हक़ीक़त है.
(बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए आप यहां क्लिक कर सकते हैं. आप हमें फ़ेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं.)